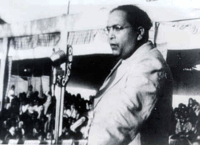Wednesday, June 22, 2011
आवागमन का सिद्धांत दलितों के आक्रोश को कुचलने के लिए बनाया गया था
क्या आपने कभी सुना है कि किसी सवर्ण के बालक ने बताया हो कि पिछले जन्म में वह दलित-वंचित था और उसे सवर्णों ने बहुत सताया। दलितों में और कमज़ोर वर्गों में जब दबंगों के विरूद्ध आक्रोश पनपा तो उन्हें शांत करने के लिए यह अवधारणा बनाई गई। इससे यह बताया गया कि अपनी हालत के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। तुमने पिछले जन्म में पाप किए थे इसलिए शूद्र बनकर पैदा हुए। अब हमारी सेवा करके पुण्य कमा लो तो अगला जन्म सुधर जाएगा।
बाबा साहब ने संघर्ष का मार्ग दिखाया और लोग जब चले उस मार्ग पर तो इसी जन्म में ही दलितों का हाल सुधर गया। यह सब व्यवस्थाजन्य खराबियां थीं। जिनका ठीकरा दुख की मारी जनता के सिर ही फोड़ डाला चतुर चालाक ब्राह्मणों ने। अब अपनी कुर्सी हिलती देखकर नई नई लीलाएं रचते रहते हैं ये।
ये तो पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दें, यह तो फिर भी बोलने वाला बालक है।
अगर पाप पुण्य का फल संसार में बारंबार पैदा होकर मिलता है तो जाति व्यवस्था को जन्मना मानने वाला और अपने से इतर अन्य जातियों को घटिया मानने वाला कोई भी नर-नारी स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। वह ब्लॉगिंग तो कर सकता है परंतु उसे यहीं जन्म लेना होगा और यहां जन्म होता नहीं है। यह एक भ्रम है जिसे सुनियोजित ढंग से फैलाया गया है। यही कारण है कि यह सिद्धांत भारत के दर्शनों में ही पाया जाता है।
Tuesday, October 26, 2010
क्या यही है हिन्दू देवताओं का दिव्य देवत्व ?
 समर्पण
समर्पणडा. अम्बेडकर के इस संसार से विदा होने पर मेरे सार्वजनिक जीवन का आरम्भ हुआ। चालीस वर्ष पूर्व, जब ,
मैंने 6 दिसम्बर,1956 को सरकारी नौकरी त्याग कर अम्बेडकर-मिशन के प्रचार व प्रसार का बीड़ा उठाया तो यह गुमान भी न था कि मार्ग इतना कठिन है, ऐसा ख़तरनाक और दुखदायक है।
इन वर्षों में वह कौन सी आफ़त है जो मुझ पर नहीं टूटी। हवालात व जेल के दुख झेले, सरकारी और ग़ैर सरकारी मुक़द्दमों की परेशानियां सहन कीं। कभी अपनों का परायापन, कभी साथियों का विश्वासघात, तो कभी साधनहीनता के थपेड़े। यही सदा महसूस हुआ कि सुख-चैन मिलने का नहीं।
कुछ ही वर्षों में वह दौर बीत गया, फिर एक नया दौर शुरू हुआ, कर्तव्य पालन के इश्क ने संघर्ष से मुहब्बत पैदा की, विपरीत हालात ने दृढ़ता को जन्म दिया,दृढ़ता ने साहस को और फिर साहस ने सुख और दुख के बीच के सभी भेद मिटा डाले -
दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है
मौत मिले तो मुफ़्त न लूं हस्ती की क्या हस्ती है
फ़ानी बदायंूनी
इस अवस्था तक पहुंचने में जिस ने मेरा हाथ स्नेहपूर्ण मजबूती से निरन्तर थामे रखा जिन्होंने बंगलूर(कर्नाटक राज्य)
में भीमराव अम्बेडकर की याद को चिरस्थायी बनाने और साधनहीन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मैडिकल, डेंटल और इंजिनियरिंग कालेजों, स्कूलों, अनेकों होस्टलों की स्थापना की, अपने उसी
गुरूभाई श्री एल. शिवालिंगईया साहिब
को यह रचना सादर समर्पित है।
- पृ. सं. 3 , हिन्दुइज्म , धर्म या कलंक ? लेखक मुद्रक व प्रकाशक ; एल. आर. बाली , संपादक भीम पत्रिका, ईएस 393 ए आबादपुरा , जालंधर 144003
अध्याय दो
नायक नहीं, खलनायक
विष्णु और कुत्ते में कोई अंतर नहीं
स्वसंवेद उपनिषद् में इस प्रकार कहा गया है-
संस्कृत में मूलसूत्र
पुनर्भवनं नो इहास्ति ... आगमपुराणेतिहासन्धर्मशास्त्रेषु! यत्तानि तु मुगध-तरमुनिशब्दवाच्यैः जीवबुद्धवुदैरचितानि भवन्ति कालकर्मात्मकमिंद स्वभावत्मक चेति न सुकृत नो दुष्कृतम्। पुष्पितवचनेन मोहितास्रे भवन्ति। केचिद् क्यं देवानुग्रहवतुः यत्र विरंचि विष्णुरूद्रा ईश्वरश्च गच्छन्ति तत्रैव ‘वानो गदर्भाः मार्जाराः कृमयश्च।
-संस्कृति संस्थान, ख्वाजा कुतुब (वेद नगर) बरेली द्वारा प्रकाशित
श्री एम.एन. राय ने अंग्रेज़ी में इसका अनुवाद इस प्रकार किया है-
"There is no incarnation, no God , no heaven , no hell , all traditional religious literature is the work of conceited fools , Nature , The organiser , and time the destoyer , are the rules of things and take no account of virtue and vice , in awarding happiness or misery to men people deluded by flowery speeches cling God's temples and priests when in reality , there is n
हिन्दी अनुवाद
न कोई अवतार होता है, न परमात्मा है और न ही स्वर्ग या नर्क है। धर्मग्रन्थ अभिमानी-मूर्खों द्वारा रचे गए हैं। स्वभाव और काल सब वस्तुओं के शासक हैं। वे मनुष्यों को सुख या दुख प्रदान करने के लिए पापों या पुण्यों पर विचार नहीं करते। लफ़्फ़ाज़ी से मोहित लोग ही देव मंदिरों और पण्डे-पुरोहितों के पीछे जाते हैं क्योंकि असल में विष्णु और कुत्ते में कोई अन्तर नहीं है।
»»»»»»
हिन्दू पुरोहिताई के विरूद्ध विद्रोह करने और उसकी खिल्ली उड़ाने वाला कोई मार्टन लूथर नहीं पैदा कर सके। न वे कोई सच्चा क्रान्तिकारी ही पैदा कर सकेह हैं। ऐसा क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर प्रो. डिके ने निम्नलिखित ‘ाब्दों में दिया है-
‘‘कभी-कभी लोग यह सवाल पूछते हैं कि पोप यह अथवा वह सुधार क्यों नहीं करता ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो पुरूष क्रान्तिकारी होता है वह पोप नहीं बनता और जो पोप बन जाता है उसमें क्रान्तिकारी बनने की कोई इच्छा नहीं होती।‘‘
श्री कृष्ण ने गीता में कहा है-
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनः।
सा यत्प्रमाणं कुरूते लोकस्तदनुवत्र्तते ।। 3-21 ।।
अर्थातः एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो कुछ करता है उसी को दूसरे लोग भी करते हैं और जिस आदर्श को वह खड़ा करता है उसी का अनुसरण जनता करती है। तात्पर्य यह कि बड़ों के आचरण छोटों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन जाते हैं।
क्या हिंदुओं को आगामी पृष्ठों में दिए अपने श्रेष्ठ व्यक्तियों यानि उनके धर्म-नायकों का अनुकरण करना चाहिए ? क्या उनका आचरण अनुकरण योग्य है ? विचारिए कि यह महापुरूष गौरव का कारण हैं अथवा लज्जा का ? यदि लज्जा का तो इनका त्याग क्यों नहीं करते ?
हिन्दू धर्मशास्त्र रचयिता और उनके नायक कितने दुराचारी थे, इस सम्बंध में कुछ लिखने की बजाए विभिन्न हिन्दू ग्रन्थों के उदाहरण देना ज़्यादा ठीक समझता है। निम्नलिखित उदाहरणों से पाठकों को उनके चरित्र व व्यवहार का भलीभांति ज्ञान हो जाएगा-
1. अहल्या से संगम करने वाला इन्द्र
गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्द्र के बारे में लिखा है कि - ‘काक समान पाप रीतौ छली मलीन कतहूं न प्रतीतो‘ अर्थात इन्द्र का तौर तरीका काले कौए का सा है, वह छली है। उसका हृदय मलीन है तथा किसी पर वह विश्वास नहीं करता। वह अश्वमेध के घोड़ों को चुराया करता था। इन्द्र ने गौतम की धर्मपत्नी अहल्या का सतीत्व अपहरण किया था। कहानी इस प्रकार है-
शचीपति इन्द्र ने आश्रम से इन्द्र की अनुपस्थिति जानकर और मुनि का वेष धारण कर अहल्या से कहा ।। 17 ।। हे अति सुन्दरी! कामीजन भोगविलास के लिए ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते, अर्थात इस बात का इन्तज़ार नहीं करते कि जब स्त्री मासिक धर्म से निवृत हो जाए तभी उनके साथ समागम करना चाहिए। अतः हे सुन्दर कमर वाली! मैं तुम्हारे साथ प्रसंग करना चाहता हूं ।। 18 ।। विश्वामित्र कहते हैं कि हे रामचन्द्र! वह मूर्खा मुनिवेशधारी इन्द्र को पहचान कर भी इस विचार से कि देखूं देवराज के साथ रति करने में कैसा दिव्य आनन्द प्राप्त होता है, इस पाप कर्म के करने में सहमत हो गई ।। 19 ।। तदनंतर वह वह कृतार्थ हृदय से देवताओं में श्रेष्ठ इन्द्र से बोली कि हे सुरोत्तम! मैं कृतार्थ हृदय से अर्थात दिव्य-रति का आनन्दोपभोग करने से मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया। अब, हे प्रेमी! आप यहां से शीघ्र चले जाइये ।। 20 ।। हे सुन्दर नितम्बों वाली! मैं पूर्ण सन्तुष्ट हूं। अब जहां से आया हूं, वहां चला जाऊँगा। इस प्रकार अहल्या के साथ संगम कर वह कुटिया से निकल गया।
2. वृन्दा का सतीत्व लूटने वाला विष्णु
विष्णु ने अपनी करतूतों का सर्वश्रेष्ठ नमूना उस समय दिखलाया जब वे असुरेन्द्र जालन्धर की स्त्री वृन्दा का सतीत्व अपहरण करने में तनिक भी नहीं हिचके। उसको वरदान था जब तक उसकी स्त्री का सतीत्व अक्षुण बना रहेगा, तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकेगा। पर वह इतना अत्याचारी निकला कि उसके लिए विष्णु को परस्त्रीगमन जैसे घृणित उपाय का आश्रय लेना पड़ा।
रूद्र संहिता युद्ध खंड, अध्याय 24 में लिखा है -
विष्णुर्जलन्धरं गत्वा दैत्यस्य पुटभेदनम् ।
अर्थात : विष्णु ने जलन्धर दैत्य की राजधानी जाकर उसकी स्त्री वृन्दा सतीव्रत्य (पतिव्रत्य) नष्ट करने का विचार किया।
इधर शिव जलन्धर कि साथ युद्ध कर रहा था और उधर विष्णु महाराज ने जलन्धर का वेष धारण कर उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट कर दिया, जिससे वह दैत्य मारा गया। जब वृन्दा को विष्णु का यह छल मालूम हुआ तो उसने विष्णु से कहा-
धिक् तदेवं हरे शीलं परदाराभिगामिनः।
ज्ञातोऽसि त्वं मयासम्यङ्मायी प्रत्यक्ष तपसः।।
अर्थात् : हे विष्णु ! पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले, तुम्हारे ऐसे आचरण पर धिक्कार है। अब तुम को मैं भलीभांति जान गई। तुम देखने में तो महासाधु जान पड़ते हो, पर हो तुम मायावी, अर्थात महाछली।
3. मोहिनी के पीछे दौड़ने वाला कामी- शिव शंकर
भगवान (?) शंकर ने दौड़कर क्रीड़ा करती हुई मोहिनी को ज़बरदस्ती पकड़ लिया। इसके बाद क्या हुआ ? महादेव शिव शंकर की तत्कालीन दयनीय अवस्था का चित्र देखना हो तो श्रीमद्भागवत, स्कन्द 8, अध्याय 12, देखने का कष्ट करें जिसमें लिखा है-
आत्मानं मोचयित्वाङग सुरर्षभभजान्तरात्।
प्रादवत्सापृथु श्रोणी माया देवविनिम्र्मता ।। 30 ।।
तस्यासौ पदवीं रूद्रो विष्णोरद्भुत कम्मर्णः।
प्रत्यपदत्तकामेन वैदिणेव निनिर्जितः ।। 31 ।।
तस्यानुधावती रेतश्चल्कन्दार्माघरेतसः।
शुष्मिणो यूथपस्येव वासितामनु धावतः ।। 32 ।।
अर्थात् : हे महाराजा ! तदन्तर देवों में श्रेष्ठ शंकर के दोनों बाहुओं के बीच से अपने को छुड़ाकर वह नारायणनिर्मिता विपुक्ष नितंबिनी माया (मोहिनी) भाग चली।। 30 ।। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी भी विचित्र चरित्र वाले विष्णु का मायामय मोहिनी रूप के पीछे-पीछे दौड़ने लगे ।। 31 ।। पीछा करते-करते ऋतुमती हथिनी के अनुगामी हाथी की तरह अमोघवीर्य महादेव का वीर्य स्खलित होने लगा ।। 32 ।।
4. अपनी बेटी से बलात्कार करने वाला, जगत रचयिता : ब्रह्मा
‘ब्रह्मा‘ शब्द के विविध अर्थ देते हुए श्री आप्टे के संस्कृत-अंग्रेजी कोष में यह लिखा है -
"Mythologically Brahma is represented as being born in a lotus ' which spran from navel of Vishnu and as a creating the world by an illicit connection with his own daughter saraswati . Brahma had originally five heads , but one of them was cut down by Shiva with his ringfinger or burnt down by the fire from the third eye ."
अर्थात् : पुराणानुसार ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुई बतलाई गई है। उन्होंने अपनी ही पु़त्री सरस्वती के साथ अनुचित संभोग कर इस जगत की रचना की। पहले ब्रह्मा के पांच सिर थे, किन्तु शिव ने उनमें से एक को अपनी अनामिका से काट डाला व अपनी तीसरी आंख से निकली हुई ज्वाला से जला दिया।
श्रीमद्भागवत, तृतीय स्कन्ध, अध्याय 12 में लिखा है-
वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयभूर्हरतीं मनः।
अकामां चकमे क्षत्रः सकाम इति नः श्रुतम्।। 28 ।।
तमधर्मे कृतमति विलोक्य पितरं सुताः।
मरीचि मुख्या मुनयो विश्रंभत प्रत्यबोधयन्।। 29 ।।
अर्थात् : मैत्रेय कहते हैं कि हे क्षता (विदुर) ! हम लोगों ने सुना है कि ब्रह्मा ने अपनी कामरहित मनोहर कन्या सरस्वती की कामना कामोन्मत होकर की ।। 28 ।। पिता की अधर्म बुद्धि को देखकर मरीच्यादि मुनियों ने उन्हें नियमपूर्वक समझाया।। 29 ।।
यह पतन की चरम सीमा नहीं ? इस से भी ज्यादा लज्जाजनक क्या कुछ और हो सकता है ?
5. गर्भवती ममता से भोग करने वाला गुरू : बृहस्पति
‘गुरू‘ शब्द का अर्थ है ‘गृणति धर्ममुपदिशतीति गुरू‘ (गृ ग कु, धे) अर्थात जो धर्म का उपदेश देता है वह गुरू है।
बृहस्पति इन्द्र आदि देवताओं का गुरू माना जाता है। इन्हीं की रची हुई एक स्मृति भी है जो बृहस्पति स्मृति के नाम से प्रसिद्ध है। ये अपने बड़े भाई उतथ्य की गर्भवती स्त्री ममता के लाख मना करने पर कामोन्मत्त होकर उस पर चढ़ बैठा।
श्रीमद्भागवत, स्कन्ध 1, अध्याय 20, में इस संबंध में इस प्रकार लिखा है-
तस्यैव वितथे वंशे तदर्थ यजतः सुतम्।
मरूतसोमेन मरूतो भरद्वाजमुपाददुः ।। 35 ।।
आन्तर्वल्र्या भ्रातृपत्न्यां मैथुनाय बृहस्पतिः।
प्रवृत्तो वारिंतो गर्भ शप्त्वा वीर्यमवासृजत्।। 36 ।।
तंप्रयुक्ताकामां ममतां भर्तृत्याग बिर्शकिताम्।
नाम निर्वचनंतस्य ‘लोकमेन सुराजगुः ।। 37 ।।
मूढ़े भारद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते।
यादौ यदुक्त्वा पितरौ भारद्वाजस्ततत्वमम्।। 38 ।।
चोद्यमाना सुरैरेवं मत्वाधित्रथमात्मजम् ।
व्यासृजत्मरूतो विभ्रन्दत्तोऽप वितथेऽन्यये ।। 39 ।।
अर्थात् : स्ववंश ने इस प्रकार नष्ट हो जाने पर राजा भरत ने मरूतसोम नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में मरूत् देवों ने राजा को भारद्वाज नामक पुत्र दिया ।। 35 ।। एक समय बृहस्पति कामातुर होकर अपने भाई की गर्भवती स्त्री के साथ मना किये जाने पर भी, मैथुन करने में प्रवृत्त हुए और गर्भ को शाप देकर अपना वीर्य छोड़ दिया ।। 36 ।। - पृ. सं. 154 से लेकर 160 पर्यन्त
अधिक प्रमाण के लिए यह भी देखा जा सकता है और फिर पूछिए अपने आप से कि क्या यही है हिन्दू देवताओं का दिव्य देवत्व ?
http://truereligiondebate.wordpress.com/2008/03/07/hindu-god-brahma-and-his-goddess-daughter-sarasvati-where-is-the-line-drawn-between-a-god-who-has-forced-sex-with-his-own-daughter-his-own-flesh-and-blood-and-runs-lusting-for-his-own-daughter-and/
Friday, October 15, 2010
पुरुष से ऊंचा स्थान है नारी का हिंदू परंपरा में ? – दीपा शर्मा

दीपा शर्मा जी
का लेख साभार प्रस्तुत है . इस लेख को प्रस्तुत करने का आशय समाज का कल्याण करना है
और यह बताना भी है कि यह लेख "शर्मा" का है किसी दलित का नहीं परन्तु यह स्त्री भी
वही कह रही है जो कि दलित चिन्तक कहते हैं . इतना अद्भुत सामी कैसे ?
आप विचार
कीजिये . सत्य सामने रखता रहेगा सत्य गौतम .
‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ का डंका पीटकर हिन्दू धर्म और संस्कृति पर गर्व करने वाले घोषणा करते हैं कि हमारे धर्म-शास्त्रों में स्त्री को देवी का रूप मानकर उसकी पूजा करने का प्रावधान है, वह इसी मनुस्मृति के तीसरे अध्याय के छप्पनवें श्लोक की पहली पंक्ति हैं। किसी ने भी यह सोचने की जरूरत नहीं समझा कि जिस मनु स्मृति ने स्त्रियों की अस्मिता को लांछित करने में कोई कोर-कसर बाक़ी न रखा हो उसमें यह श्लोक आया ही क्यों? लेकिन करें क्या, इस श्लोकार्द्ध का अर्थ ऊपर से देखने में इतना सीधा और सरल है कि इसको किसी के मन में कोई संशय ही नहीं पैदा होता। इसके अतिरिक्त यह कारण भी हो सकता है कि अधिकांश लोगों को यह पता ही न हो कि यह किस ग्रन्थ में है वास्तविक अर्थ तक कैसे पहुँचेगे। इस श्लोक को यदि श्लोक संख्या ५४ और ५५ के साथ पढ़ा जाये तो स्पष्ट होगा कि ‘पूजा’ का आशय विवाह में दिया जाने वाला स्त्री धन है और मनु ने इससे दहेज प्रथा की शुरुआत की थी। स्त्री-विमर्श के पैरोकारों को चाहिये कि वे इस दुष्टाचार का पर्दाफ़ाश करें।
‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ के द्वारा स्मृतिकार कहीं से भी यह नहीं कहना चाहता कि स्त्री पूज्यनीय है। यदि बहुप्रचारित (यद्यपि दुष्प्रचारित कहना ज्यादा सटीक है) अर्थ ही लिया जाए तो भी यह सिद्ध नहीं होता कि स्त्रियों के बारे में इससे भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व रेखांकित होता है। यह श्लोक हाईपोथीसिस की बात करता है किसी प्रकार का आदेश नहीं देता। ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी ने इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया है, ‘‘जिस कुल में स्त्रियाँ पूजित (सम्मानित) होती हैं, उस कुल से देवता प्रसन्न होते हैं।” इस अनुवाद से भी यही सिद्ध होता है कि यह एक अन्योन्याश्रित स्थिति है अर्थात् स्त्रियों को पूज्य घोषित करने का कोई बाध्यकारी आदेश नहीं दिया। मनु ने, जैसा कि उन्हें प्रताड़ित अपमानित करने के लिए आदेशित किया है। यही कारण है कि स्त्रियों के बारे में पुरुषों में अच्छी धारणा अंकुरित ही नहीं हो पायी।
मनुस्मृति ने स्त्रियों की अस्मिता और स्वाभिमान पर कितने तरीक़े से हमला किया है, उसकी बानगी देखिये-शूद्र की शूद्रा ही पत्नी होती है। वैश्य को वैश्य और शूद्र दोनों वर्ण की कन्यायों से, क्षत्रिय को क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों वर्ण की कन्याओं से तथा ब्राह्मण को चारों वर्णों की कन्याओं से विवाह करने का अधिकार है। (३.१३)
लेकिन इसके तुरन्त बाद वाला श्लोक आदेश देता है-ब्राह्मण और क्षत्रिय को स्वर्णा स्त्री न मिलने पर भी शूद्रा को स्त्री बनाने का किसी भी इतिहास में आदेश नहीं पाया जाता। (३.१४)
इसके आगे के श्लोकों में भी शूद्र वर्ण की स्त्री के लिये तमाम घिनौनी बातें कही गई हैं लेकिन निम्न श्लोक में तो सारी सीमाओं को तोड़कर रख दिया- जो शूद्रा के अधर रस का पान करता है उसके निःश्वास से अपने प्राण-वायु को दूषित करता है और जो उनमें सन्तान उत्पन्न करता है उसके निस्तार का कोई उपाय नहीं है। (३.१९)
किन्तु जैसे ही याद आया कि इससे स्त्रियों को अबाध भोगने के अधिकार से सवर्ण पुरुष वंचित हो जायेंगे तो कह दिय-स्त्रियों का मुख सदा शुद्ध होता है….(५.१३०)
अब स्त्रियों पर कुछ सामान्य टिप्पणियाँ भी देखिये-
मदिरा पीना, दुष्टों की संगति, पति का वियोग, इधर-उधर घूमना, कुसमय में सोना और दूसरों के घरों में रहना ये छः स्त्रियों के दोष है। (२.१३)
स्त्रियाँ रूप की परीक्षा नहीं करतीं, न तो अवस्था का ध्यान रखती हैं, सुन्दर हो या कुरूप हों, पुरुष होने से ही वे उसके साथ संभोग करती हैं। (९.१४)
पुंश्चल (पराये पुरुष से भोग की इच्छा) दोष से, चंचलता से और स्वभाव से ही स्नेह न होने के कारण घर में यत्नपूर्वक रखने पर भी स्त्रियाँ पति के विरुद्ध काम करती हैं। (९.१५)
ब्रह्मा जी ने स्वभाव से ही स्त्रियों का ऐसा स्वभाव बनाया है, इसलिये पुरुष को हमेशा स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। (९.१६)
मनु जी ने सृष्ट्यादि में शय्या, आसन, आभूषण, काम, क्रोध, कुटिलता, द्रोह और दुराचार स्त्रियों के लिए ही कल्पना की थी। (९.१७)
ऐसे न जाने कितने श्लोक पूरी मनु स्मृति में फैले पड़े हैं।
ऋग्वेद के मंत्र १०।८५।३७ हो या मनु स्मृति के नवें अध्याय के श्लोक ३३ से लेकर ५२ तक स्त्रियों को पुरुषों की खेती कहा गया है। इस्लाम भी कुरान की आयत १.२.१२३ के द्वारा इसी प्रकार की व्यवस्था करता है
ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी (सुं.कां. ६२-३) का उद्घोष करने वाले तुलसीदास ने भी स्त्री-निंदा में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ा। ‘सरिता’ फरवरी १९५६(सरिता मुक्ता रिप्रिंट भाग-१) के अंक में ‘रामचरितमानस में नारी’ शीर्षक से प्रकाशित लेख में इसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। ऐसा करने में उन्होंने भी मनु की शूद्र स्त्री को अलग खाने में रखा है। संदर्भित लेख से ही कुछ उद्धरणों को देकर इसे स्पष्ट किया जा रहा है- करै विचार कुबुद्धि कुजाती। होई अकाजु कवनि विधि राती।/देखि लागि मधु कुटिल किराती। जिमि गंव तकै लेऊँ केहि भाँति॥/भरत मातु पहि गइ बिलखानी। का अनमनि हसि कह हँसि रानी॥/उतरू देहि नहिं लेइ उसासू। नारि चरित करि ढारइ आँसू।
खोटी बुद्धि वाली और खोटी-नीच जाति वाली मंथरा विचार करने लगी कि रात ही रात में यह काम कैसे बिगाड़ा जाए? जिस तरह कुटिल भीलनी शहद के छत्ते को लगा देखकर अपना मौका ताकती है कि इसको किस तरह लूँ। वह बिलखती हुई भरत की माता कैकेई के पास गई। उसको देखकर कैकेई ने कहा कि आज तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ जवाब नहीं देती और लंबी साँस खींचती है और स्त्री चरित्रकरके आँखों से पानी टपकाती है।
मंथरा कैकेई के लिए ही मरती रहती है लेकिन तुलसीदास ने कैकेई के ही मुँह से उसके लिए यह कहलवाया – काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। तिय विसेखि मुनि चेरि कहि भरत मातु मुसकानि।
काने, लंगड़े, लूले – ये बड़े कुटिल और कुचाली होते हैं और उनमें भी स्त्री और विशेष रूप से दासी-ऐसा कहके भरत मातु मुसकाई।
इतने विशेषणों से उसे तब अलंकृत किया गया जबकि स्वयं सरस्वती ने उसकी मति फेरी थी, अर्थात् सरस्वती भी स्त्री होने के कारण लपेटे में। सीता और पार्वती को भी क्रमशः राम और शिव की किंकरी ही घोषित कराया है। तुलसीदास ने और वह भी उनकी माता के ही मुँह से। सीता की माँ सीता की विदाई के समय राम से कहती है – तुलसी सुसील सनेहु लखि निज किंकरी कर मानिबी।
इसके सुशील स्वभाव और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी मानियेगा। बिल्कुल यही बात पार्वती की माँ भी बेटी को विदा करते समय शिव से कहती है – नाथ उमा मम प्रान सम गृह किंकरी करेहु/छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु।
हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान है। अब इसे अपने घर की दासी बनाइये और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए-करेहु सदा संकर पद पूजा। नारि धरम पति देव न दूजा॥
पार्वती को उपदेश देते हुए कहती हैं कि हे पुत्री, तू सदा शिव के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जब ईश्वर या उसके अवतार द्वारा स्वयं ही पत्नी को अपने चरण में जगह दी जाती है तो पुरुष क्यों नहीं करेगा अथवा उसे क्यों नहीं करना चाहिए?
गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित रामचरित मानस के एक सौ छठवें संस्करण में निम्न दृष्टांत उद्धृत किए जा रहे हैं – माता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी॥/होई विकल सक मनहि न रोकी। जिमि रबि मनि द्रव रबिहि विलोकी॥ (पृष्ठ ६२६)
स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि ‘सूर्य’ को देखकर द्रवित हो जाती है।
सती अनसूया द्वारा सीता को उपदेश देते समय उनके मुँह से स्त्रियों के बारे में जो कहलवाया गया है, वह पृष्ठ संख्या ६०९ और ६१० पर अंकित है। देखिए – धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काल परिखिअहिं चारी॥/वृद्ध रोग सब जड़ धन हीना।/ अंध बधिर क्रोधी अति दीना॥/ऐसेहु पति कर किएँ अपमाना।/नारि पाव जमपुर दुखनाना॥/एकइ धर्म एक व्रत नेमा।/कायॅ वचन मन पति पद प्रेमा॥
धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री – इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यन्त ही दीन-ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भाँति-भाँति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए, बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है-जग पतिव्रता चारि विधि अहहीं। वेद पुरान संत सब कहहीं॥/उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं॥
जगत् में चार प्रकार की पतिव्रताएँ हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत् में(मेरे पति को छोड़कर) दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है-मध्यम परपति देखइ कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे॥/धर्म विचारी समुझि कुल रहईं।/सा निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहईं॥
मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो(अर्थात् समान अवस्था वाले वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है।) जो धर्म के विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं- बिन अवसर भय तें रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई॥/पति बंचक परपति रति करई। रौरव नरक कल्प सत परई॥
जो स्त्री मौका न मिलने से या भयावश पतिव्रता बनी रहती है, जगत् में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो सौ कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है-छन सुख लागि जनम सत कोटी। दुख न समुझ तेहि सम को खोटी॥/बिनु श्रम नारि परम गति लहई। पतिब्रत धर्म छाड़ि छल गहई॥
क्षणभर के सुख के लिए जो सौ करोड़ (असंख्य) जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है – पति पतिकूल जनम जहँ जाई। बिधवा होइ पाइ तरुनाई॥
किन्तु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर (भरी जवानी में) विधवा हो जाती है – सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ।/जसु गावति श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिंहि प्रिय॥
स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किन्तु पति की सेवा करके यह अनायास ही शुभगति प्राप्त कर लेती है। (पतिव्रत धर्म के कारण) आज भी ‘तुलसी जी’ भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं।
तुलसीदास जी को पुरुषों में कोई दोष नहीं दिखाई देता तो इसके पीछे पुरुष की वही स्त्री विरोधी मानसिकता है जिसे बड़े करीने से धर्मशास्त्र की सान पर परवान चढ़ाकर विकसित किया गया है और जो आज भी क़ायम है।
(मूलचंद जी के लेख से …….)
कबीर तुलसी के समकालीन माने जाते हैं : परन्तु दोनों का रचना-संसार समान नहीं है। आज कबीर को सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, शोषितों, पीड़ितों के प्रबल पक्षकार के रूप में देखा जाता है लेकिन स्त्रियों की निंदा करने में वह भी किसी से पीछे नहीं है। डॉ. युगेश्वर द्वारा सम्पादित और हिन्दी प्रचारक संस्थान वाराणसी द्वारा प्रकाशित ‘कबीर समग्र’ के प्रथम संस्करण १९९४ से कुछ साखियाँ यहाँ उद्धृत की जा रही हैं :-
कामणि काली नागणीं तीन्यूँ लोक मंझारि।
राम सनेही ऊबरे, विषई खाये झारि॥
(पृष्ठ २८४)
एक कनक अरु कॉमिनी, विष फल कीएउ पाइ।
देखै ही थै विष चढै+, खॉयै सूँ मरि जाइ॥
(पृष्ठ २८६)
नारी कुंड नरक का, बिरला थंभै बाग।
कोई साधू जन ऊबरै, सब जग मूँवा लाग॥
(पृष्ठ २८६)
जोरू जूठणि जगत की, भले बुरे का बीच।
उत्थम ते अलग रहैं, निकट रहें तें नीच॥
(पृष्ठ २८६)
सुंदरि थै सूली भली, बिरला बंचै कोय।
लोह निहाला अगनि मैं, जलि बलि कोइला होय॥
(पृष्ठ २८६)
इक नारी इक नागिनी, अपना जाया खाय।
कबहूँ सरपटि नीकसे, उपजै नाग बलाय॥
(पृष्ठ ४३७)
सर्व सोनाकी सुन्दरी, आवै बास सुबास।
जो जननी ह्नै आपनी, तौहु न बैठे पास॥
(पृष्ठ ४३७)
गाय भैंस घोड़ी गधी, नारी नाम है तास।
जा मंदिर में ये बसें, तहाँ न कीजै बास॥
(पृष्ठ ४३८)
छोटी मोटी कामिनी, सब ही विष की बेल।
बैरी सारे दाब दै, यह मारै हँसि खेल॥
(पृष्ठ ४४०)
नागिन के तो दोय फन, नारी के फन बीस।
जाको डस्यो न फिरि जिये, मरि है बिस्वा बीस॥
(पृष्ठ ४४०)
इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्री निंदा में कोई किसी से कम नहीं है।
आर्ष समाज से लेकर अर्वाचीन समाज तक स्त्रियों की छवि को एक विशेष खाँचे में फिट किया गया है, मातृ-सत्तात्मक समाज रहा हो या पितृ-सत्तात्मक स्त्री को देह की भाषा में ही व्यक्त करने और होने का खेल चलता रहा। इस खेल में स्त्री भी बराबर की हिस्सेदार रही। उसने इस आरोपण को सच की तरह अंगीकृत कर लिया कि वह एक देह है और इस देह की एक मात्र आवश्यकता है यौन-तृप्ति। यह मानते हुए भी कि यौन-सम्बन्ध द्विपक्षीय अवधारणा है जिसके प्रति पुरुष भी उतना ही लालायित रहता है। विकास के किसी भी मोड़ पर पुरुषों की काम-प्रवृत्ति का उस तरह से मनोविश्लेषण नहीं किया गया जैसा कि स्त्रियों का। इसका परिणाम यह हुआ कि सारी वर्जनाएँ स्त्रियों पर ही थोप दी गईं और पुरुषों को स्वच्छंद छोड़ दिया गया और वे स्त्रियों के साथ निर्द्वन्द्व होकर मनमानी करते रहे। स्त्रियाँ भोग्या बनने और वर्जनाओं के उल्लंघन के नाम पर लांछित होने को अभिशप्त होती रहीं। यही उनकी नियति बन गयी और उन्हीं के मुँह से इसे स्वीकार भी कराया गया। यह पुरुष-सत्तात्मक समाज के नीति-नियामकों की जीत और स्त्रियों की सबसे बड़ी हार थी, जिस पर ईश्वर की सहमति का ठप्पा भी लगवा लिया गया।
वेद, पुराण और महाभारत से उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार इन ग्रन्थों में स्त्रियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है। वेदों में वर्णित कुछ कामुक दृष्टांत हरिमोहन झा की पुस्तक ‘खट्टर काका’ से साभार लेकर यहाँ पर उद्धृत किए जा रहे हैं – मर्य इव युवतिभिः समर्षति सोमः/कलशे शतयाम्ना पथा (ऋ. ९/८६/१६)
कलश में अनेक धारों से रस का फुहारा छूट रहा है। जैसे, युवतियों में… (पृष्ठ १९४)
को वा शयुत्र विधवेव देवरं मर्यं न योषा वृणुते (ऋ. ७/४०/२)
‘‘जैसे विधवा स्त्री शयनकाल में अपने देवर को बुला लेती है, उसी प्रकार मैं भी यज्ञ में आपको सादर बुला रही हूँ। (पृष्ठ १९५)
यत्र द्वाविव जघनाधिषवरण्या/उलूखल सुतानामवेद्विन्दुजल्गुलः (ऋ. १/२८/२)
‘‘जैसे कोई विवृत-जघना युवती अपनी दोनों जंघाओं को फैलाये हुई हो और उसमें..(पृष्ठ १९३)
अभित्वा योषणो दश, जारं न कन्यानूषत/मृज्यसे सोम सातये (ऋ. ९/५६/३)
‘‘कामातुरा कन्या अपने जार (यार ) को बुलाने के लिये इसी प्रकार अंगुलियों से इशारा करती हैं। (पृष्ठ १९३ )
वृषभो न तिग्मश्रृंगोऽन्तर्यूथेषु रोरुवत्! (ऋ. १०/८६/१५)
अर्थात् ‘जिस प्रकार टेढ़ी सींग वाला साँड़ मस्त होकर डकरता हुआ रमण करता है, उसी प्रकार तुम भी मुझसे करो। (पृष्ठ १९६)
डॉ. तुलसीराम ने अपने लेख ‘बौद्ध धर्म तथा वर्ण व्यवस्था’ (‘हंस’, अगस्त २००४) में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के छठवें मंत्र का अनुवाद इस तरह किया है, ‘‘यह संभोग्य युवती (यानी जिसके गुप्तांग पर बाल उग आए हों) अच्छी तरह आलिंगन (बद्ध) होकर सूतवत्सा नकुली (यानी एक रथ हाँकने वाले की बेटी, जिसका नाम नकुली था) की तरह लम्बे समय तक रमण करती है। वह बहु-वीर्य सम्पन्न युवती मुझे अनेक बार भोग प्रदान करती हैं।” इसी लेख में यह भी कहा गया है कि ऋग्वेद के अंग्रेजी अनुवाद राल्फ टी ग्रीफिथ को दसवें मंडल के ८६ वें सूक्त के मंत्र १६ और १७ इतने वीभत्स लगे कि उन्होंने इनका अनुवाद ही नहीं किया।
ऋग्वेद के दसवें मंडल के दसवें सूक्त में सहोदर भाई-बहन यम और यमी का संवाद है जिसमें यमी यम से संभोग याचना करती है। इसी मंडल के ६१ वें सूक्त के पाँचवें-सातवें तथा अथर्ववेद (९/१०/१२) में प्रजापति का अपनी पुत्री के साथ संभोग वर्णन है। यम और यमी के प्रकरण का विवरण अथर्ववेद के अठारहवें कांड में भी मिलता है। (भारतीय विवाह संस्था का इतिहास – वि.का. राजवाडे, पृष्ठ ९७) इसी पुस्तक के पृष्ठ ७८-७९ पर पिता-पुत्री के सम्बन्धों पर चर्चा करते हुए वशिष्ठ प्रजापति की कन्या शतरूपा, मनु की कन्या इला, जन्हू की कन्या जान्हवी (गंगा) सूर्य की पुत्राी उषा अथवा सरण्यू का अपने-अपने पिता के साथ पत्नी भाव से समागन होना बताया गया है। ‘स्त्री-पुरुष समागम सम्बन्धी कई अति प्राचीन आर्ष प्रथाएँ नामक यह अध्याय सगे-सम्बन्धियों के मध्य संभोग-चर्चा पर आधारित है। इस प्रकार के सम्बन्धों की चर्चा महाभारत के ‘शांतिपूर्व’ के २०७ वें अध्याय के श्लोक संख्या ३८ से ४८ तक में भीष्म द्वारा की गई है। राजवाडे ने अपनी उक्त संदर्भित पुस्तक के पृष्ठ ११५-११६ पर (श्लोक का क्रम ३७ से ३९ अंकित है।) इन श्लोकों का अर्थ निम्नवत् किया है- कृतयुग (संभवतः सतयुग) में स्त्री-पुरुषों के बीच, जब मन हुआ तब, समागम हो जाता था। माँ, पिता, भाई, बहन का भेद नहीं था। वह यूथावस्था थी। (श्लोक सं. ३८) त्रेता युग में स्त्री-पुरुषों द्वारा एक-दूसरे को स्पर्श करने पर समाज उन्हें उस समय के लिए संभोग करने की अनुमति देता था। यह पसन्द-नापसन्द या प्रिय-अप्रिय का चुनाव करने की व्यवस्था थी। (श्लोक सं. ३९) द्वापर युग में मैथुन धर्म शुरू हुआ। इस पद्धति के अनुसार, स्त्री-पुरुष अपनी टोली में जोड़ियों में रहने लगे, किन्तु अभी भी इन जोड़ियों को स्थिर अवस्था प्राप्त नहीं हुई थी और कलियुग में द्वंद्वावस्था की परिणति हुई, अर्थात् जिसे हम विवाह संस्था कहते हैं उसका उदय हुआ। (श्लोक सं. ४०)
‘खट्टर काका’ के पृष्ठ ६४ पर भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग खंड के हवाले से उद्धृत निम्न श्लोक की मानें तो ईश्वरीय सत्ता के तीनों शीर्ष प्रतीक भी इस स्वच्छन्द सम्बन्ध से मुक्त नहीं हैं-स्वकीयां च सुतां ब्रह्मा विष्णुदेवः स्वमातरम्/भगनीं भगवान् शंभुः गृहीत्वा श्रेष्ठतामगात्!
स्त्री के मुँह से ही स्त्रियों की बुराई सिद्ध करने के आख्यान मिलते हैं। स्त्रियों का यह चरित्र- चित्राण उनकी विश्व-विख्यात ईर्ष्या-भावना की छवि को उद्घाटित करता है। इस प्रकार का एक दृष्टांत महाभारत से यहाँ पर उद्धृत है। आगे, सम्बन्धित खंड में रामरचितमानस से भी ऐसा ही दृष्टांत उद्धृत किया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अन्तर्गत ‘दानधर्म’ पर्व में पंचचूड़ा, अप्सरा और नारद के मध्य एक लम्बा संवाद है, जिसमें पंचचूड़ा स्त्रियों के दोष गिनती है। इसमें से कुछ श्लोकार्थ यहाँ दिये जा रहे हैं-नारद जी! कुलीन, रूपवती और सनाथ युवतियाँ भी मर्यादा के भीतर नहीं रहतीं। यह स्त्रियों का दोष है॥११॥ प्रभो! हम स्त्रियों में यह सबसे बड़ा पातक है कि हम पापी पुरुषों को भी लाज छोड़कर स्वीकार कर लेती हैं॥१४॥ इनके लिये कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है, जो अगम्य हो। इनका किसी अवस्था-विशेष पर भी निश्चय नहीं रहता। कोई रूपवान हो या कुरूप; पुरुष है- इतना ही समझकर स्त्रियाँ उसका उपभोग करती हैं॥१७॥ जो बहुत सम्मानित और पति की प्यारी स्त्रियाँ हैं; जिनकी सदा अच्छी तरह रखवाली की जाती है, वे भी घर में आने-जाने वाले कुबड़ों, अन्धों, गूँगों और बौनों के साथ भी फँस जाती है॥२०॥ महामुनि देवर्षे! जो पंगु हैं अथवा जो अत्यन्त घृणित मनुष्य (पुरुष) हैं, उनमें भी स्त्रियों की आसक्ति हो जाती है। इस संसार में कोई भी पुरुष स्त्रियों के लिये अगम्य नहीं हैं॥२१॥ ब्रह्मन! यदि स्त्रियों को पुरुष की प्राप्ति किसी प्रकार भी सम्भव न हो और पति भी दूर गये हों तो वे आपस में ही कृत्रिम उपायों से ही मैथुन में प्रवृत्त हो जाती हैं॥२२॥ देवर्षे! सम्पूर्ण रमणियों के सम्बन्ध में दूसरी भी रहस्य की बात यह है कि मनोरम पुरुष को देखते ही स्त्री की योनि गीली हो जाती है॥२६॥ यमराज, वायु, मृत्यू, पाताल, बड़वानल, छुरे की धार, विष, सर्प और अग्नि – ये सब विनाश हेतु एक तरफ और स्त्रियाँ अकेली एक तरफ बराबर हैं॥२९॥ नारद! जहाँ से पाँचों महाभूत उत्पन्न हुए हैं, जहाँ से विधाता ने सम्पूर्ण लोकों की सृष्टि की है तथा जहाँ से पुरुषों और स्त्रियों का निर्माण हुआ है, वही से स्त्रियों में ये दोष भी रचे गये हैं (अर्थात् ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं।)॥३०॥
इस आख्यान से दो बातें स्पष्ट सिद्ध होती है। पहली एक ही स्रोत से रची गई चीजों में विधाता ने मात्र स्त्रियों के लिये ही दोषों की रचना करके पक्षपात किया और दूसरी यह कि स्वयं विधाता ही पुरुष-वर्चस्व का पोषक है।
मूलचंद जी के लेख से आगे जारी रखते हुए …….
हमारे शास्त्र कन्या-संभोग और बलात्कार के लिये भी प्रेरित करते हैं। मनुस्मृति के अध्याय ९ के श्लोक ९४ में आठ वर्ष की कन्या के साथ चौबीस वर्ष के पुरुष के विवाह का प्रावधान है। ‘भारतीय विवाह का इतिहास’(वि.का. राजवाडे) के पृष्ठ ९१ पर उद्धृत वाक्य ‘‘चौबीस वर्ष का पुरुष, आठ वर्ष की लड़की से विवाह करे, इस अर्थ में स्मृति प्रसिद्ध है। विवाह की रात्रिा में समागम किया जाय, इस प्रकार के भी स्मृति वचन हैं। अतः आठ वर्ष की लड़कियाँ समागमेय हैं, यह मानने की रूढ़ि इस देश में थी, इसमें शक नहीं।” इसी पुस्तक के पृष्ठ ८६-८७ तथा ९० के नीचे से चार पंक्तियों को पढ़ा जाय तो ज्ञात होता है कि कन्या के जन्म से लेकर छः वर्ष तक दो-दो वर्ष की अवधि के लिये उस पर किसी न किसी देवता का अधिकार होता था। अतः उसके विवाह की आयु का निर्धारण आठ वर्ष किया गया। क्या इससे यह संदेश नहीं जाता कि कन्या जन्म से ही समागमेय समझी जाती थी क्योंकि छः वर्ष बाद उस पर से देवताओं का अधिकार समाप्त हो जाता था। यम संहिता और पराशर स्मृति दोनों ही रजस्वला होने से पूर्व कन्या के विवाह की आज्ञा देते हैं (खट्टर काका पृष्ठ १०१) निम्न श्लोक देखें-प्राप्ते तु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति/मासि मासि रजस्तयाः पिब्रन्ति पितरोऽनिशम्। (यम संहिता)
यदि कन्या का विवाह नहीं होता और यह बारह वर्ष की होकर रजस्वला हो जाती है तो उसके पितरों को हर माह रज पीना पड़ेगा-रोमकाले तु संप्राप्ते सोमो सुंजीथ कन्यकाम/रजः काले तुः गंधर्वो वद्दिस्तु कुचदर्शने।
रोम देखकर सोम देवता, पुष्प देखकर गंधर्व देवता और कुच देखकर अग्नि देवता कन्या का भोग लगाने पहुँच जायेंगे।
जिस धर्म के देवता इतने बलात्कारी, उस धर्म के अनुयायी तो उनका अनुसरण करेंगे ही। कुंती के साथ सूर्य के समागम का विवरण राजवाडे के शब्दों में इस प्रकार है,-’वनपर्व’ के ३०७वें अध्याय में सूर्य कहता है- ‘‘हे कुंती, कन्या शब्द की उत्पत्ति, कम् धातु से हुई और इसका अर्थ है- चाहे जिस पुरुष की इच्छा कर सकने वाली। कन्या स्वतंत्र है, स्त्रियों और पुरुषों में किसी प्रकार का परदा या मर्यादा न होना- यही लोगों की स्वाभाविक स्थिति है, विवाहादि संस्कार सब कृत्रिम हैं, अतः तुम मेरे साथ समागम करो, समागम करने के बाद तुम पुनरपि कुमारी ही, अर्थात् अक्षत योनि ही रहोगी।” (वही, पृष्ठ ८९-९०) और देवराज इन्द्र द्वार बलात्कार के किस्से तो थोक के भाव मौजूद है।
यह रहा, तथाकथित पूज्य वेदों, पुराणों, महाभारत इत्यादि का स्त्रियों के प्रति रवैये की छोटी-सी बानगी। संस्कृत वाङ्मय के ग्रन्थ अथवा साहित्यिक रचनायें अथवा उनसे प्रेरित श्रृंगारिक कवियों की श्रृंगारिक भाषायी रचनाओं से लेकर आधुनिकता का लिबास ओढ़े चोली के पीछे क्या है…. ‘अथवा’ मैं चीज बड़ी हूँ मस्त-मस्त….. तक के उद्घोष में स्त्री-पुरुष बराबर के साझीदार हैं। इन कृतियों में से होकर एक भी रास्ता ऐसा नहीं जाता जिस पर चलकर स्त्री सकुशल निकल जाये, फिर भी वह इनके प्रति सशंकित नहीं है तो इस पर गहन, गम्भीर विमर्श होना चाहिये। सबसे बड़ी विडम्बना तो स्त्रियों का कृष्ण के प्रति अनुराग है जबकि स्त्रियों के साथ कृष्ण-लीला इनके चरित्र का सबसे कमजोर पहलू है। ब्रह्म वैवर्त में कृष्ण का राधा या अन्य गोपियों के साथ संभोग का जैसा वर्णन है, उसको पढ़कर उनके आचरण को अध्यात्म की भट्ठी में चाहे जितना तपाया जाये, उसे नैतिकता के मापदण्ड पर खरा नहीं ठहराया जा सकता।
मनु स्मृति संभवतः ऐसा अकेला ग्रन्थ है जिनसे भारतीय मेधा को न केवल सबसे अधिक आकर्षित किया अपितु व्यवहार-जगत् में उसकी मानसिकता को ठोस एवं स्थूल स्वरूप भी प्रदान किया। भारतीय मेधा अर्थात् भारतीय राज्य-सत्ता और उसके द्वारा पोषित सामंती प्रवृत्तियों का गंठजोड़, जिसके हाथ में मनु ने मनुस्मृति के रूप में, ‘करणीय और अकरणीय’ का औचित्य-विहीन संहिताकरण करके एक क्रूर और अमानवीय हथियार पकड़ा दिया और उसे धर्म-सम्मत मनमानी करने का निर्णायक अवसर प्रदान कर दिया। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मनुस्मृति का सबसे घातक दुष्परिणाम यह हुआ कि इसने पहले से ही क्षीण होती जा रही संतुलन-शक्तियों का समूल विनाश कर दिया। शूद्र (वर्तमान दलित) और स्त्री के लिये दंड-विधान के रूप में ऐसे-ऐसे प्रावधान किये गये कि इनका जीवन नारकीय हो गया।
विषय-वस्तु के बेहतर प्रतिपादन के लिये थोड़ा विषयान्तर समीचीन दिखता है। मनु-स्मृति में हमें तीन बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं। पहला, वर्ण-व्यवस्था का पूर्ण विकसित और अपरिवर्तनीय स्वरूप (मनु १०.४) दूसरा, राक्षस या असुर जाति का विलोपीकरण और तीसरा देवताओं के अनैतिक आचरण को विस्थापित करके उनकी कल्याणकारी इतर शक्तियों के रूप में स्थापना। वर्ण-व्यवस्था का सिद्धान्त आर्यों की देन है जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से प्रारम्भ होता है और सभी अनुवर्ती ग्रन्थों में जगह पाता है। स्त्रियों की भाँति राक्षसों की भी उत्पत्ति वर्ण-व्यवस्था से नहीं होती। सुर और असुर के मध्य लड़े गये तमाम युद्धों का वर्णन वैदिक साहित्य में भरे पड़े हैं। रामायण काल तक राक्षस मिलते हैं, महाभारत काल में विलुप्त हो जाते हैं। महाभारत काल में कृष्ण के रूप में ईश्वर अवतार लेते हैं। गीता में अपने अवतार का कारण अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना बताते हैं। प्रत्यक्ष विनाश वे अपने मामा कंस का करते है। महाभारत युद्ध की विनाश-लीला के नायक होते हुए भी इस युद्ध में उनकी भूमिका राम की तरह नहीं है। कृष्ण का मामा होने के कारण कंस को राक्षस कहा जाय तो सबसे बड़ी अड़चन यह आयेगी कि कृष्ण को भी राक्षस कहना पड़ेगा लेकिन थोड़ा-सा ध्यान दें तो इस गुत्थी को सुलझाना बहुत आसान है। राम और रावण के बीच लड़ा गया युद्ध निश्चित रूप से आर्यों के बीच लड़ा गया अन्तिम महायुद्ध था जिसमें आर्यों की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय यह थी कि आर्य राम की सेना अनार्य योद्धाओं की थी और रावण की पारिवारिक कलह चरम पर थी। इसका प्रत्यक्ष लाभ राम को यह मिला कि उन्हें घर का भेदी ही मिल गया और लंका ढह गयी। आर्य संस्कृति की विजय हुई लेकिन वर्चस्व स्थापित नहीं हो सका होगा। क्योंकि विभीषण चाहे जितना बड़ा राम भक्त राह हो, तो अनार्य ही न और फिर रावण की पटरानी मंदोदरी ही उसकी पटरानी बनी। क्या विभीषण कभी उससे आँख मिला पाया होगा? क्या कभी मंदोदरी यह भुला सकी होगी कि वह जिस कायर की पत्नी है उसी के विश्वासघात ने उसके प्रतापी पति की हत्या करवाई थी।
इस कड़ी को कृष्ण द्वारा कंस के संहार से जोड़कर देखें तो स्थिति यह बनती है कि अनार्यों की बची-खुची शक्ति के सम्पूर्ण विनाश के लिये इस बार घर से ही नायक को उठाया गया। यह इस बात से सिद्ध है कि कृष्ण के नायकत्व या संयोजकत्व में जितने भी युद्ध लड़े गये सभी पारिवारिक थे। अतः यह कहा जा सकता है कि अनार्य आपस में लड़कर विनाश को प्राप्त हुए और वर्ण से बाहर की दलित जातियाँ उन्हीं की ध्वंसावशेष हैं। इस सम्पूर्ण विजय के बाद आचरण हीन देवता स्वयं को कल्याणकारी इतर शक्ति के रूप में स्थापित कराने में सफल हो गये तो क्या आश्चर्य।
मनु स्मृति शांति काल की रचना प्रतीत होती है जिसमें शासन-व्यवस्था के संचालन और समाज को नियंत्रित करने का प्रावधान है। स्पष्ट है कि इसका डंडा वर्णेतर जातियों पर पड़ना था और पड़ा भी। दलित और स्त्री उन सभी सुविधाओं और अवसरों से वंचित कर दिये गये जो उनके बौद्धिक-क्षमता के विकास में सहायक थे। इस प्रकार मनु स्मृति से भी यह सिद्ध होता है कि दलित और स्त्री वर्ण-व्यवस्था के बाहर का समुदाय है।
मूलचंद जी के लेख से कुछ आगे जारी रखते हुए …….
अभी तो मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि स्त्री मर जाती है, स्त्री पैदा होती है लेकिन उसके दुर्गति की शाश्वतता बनी रहती है। इंतजार है नई स्त्री के पैदा होने की जो विद्रोह कर सके। ब्रह्मा, विष्णु और शिव हिन्दू धर्म में ईश्वर की तीन सर्वोच्च प्रतीक हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति, विष्णु पालन और शिव संहार के देवता माने गये हैं। इस रूप में ये एक-दूसरे के पूरक दिखते हैं लेकिन वैष्णवों के मध्य हुए संघर्षों से यह सिद्ध होता है कि प्रारम्भ के किसी काल-खंड में शिव और विष्णु एक-दूसरे के विरोधी विचारधारा के पोषक और संवाहक थे। पालक होते हुए भी तथाकथित अधर्मियों का विनाश करने के लिए विष्णु ही बार-बार अवतार लेते हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती इनकी पत्नियों के नाम हैं। आइये देखें कि यौन-विज्ञान के महारथियों ने इनका किस प्रकार चित्रण किया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का सरस्वती, लक्ष्मी और पर्वती के साथ पत्नी के अतिरिक्त अन्य सम्बन्ध का उल्लेख इस लेख के दूसरे खंड में किया जा चुका है। आगे बढ़ने से पूर्व स्त्रियों के प्रति इस वीभत्स काम-कुंठा की अभद्र मानसिकता की एक बानगी देखिये जो ‘खट्टर काका’ के अन्तिम पृष्ठ पर अथर्ववेद के हवाले से उद्धृत किया गया है-यावर्दैीनं पारस्वतं हास्तिनं गार्दभं च यत्/यावदश्वस्य वाजिनस्तावत् से वर्धतां पसः। (अथर्व ६/७२/३)
अर्थात् ‘‘कामदंड बढ़कर वैसा स्थूल हो जाय जैसा हाथी, घोड़े या गधे का…।”
इस लम्पट और उद्दंड कामुकता के वेग का प्रभाव ऐसा पड़ा यहाँ के यौनाचार्यों पर कि देवी तक की वंदना करते समय उनके कामांगों का स्मरण करना नहीं भूलते। उदाहरण-वामकुचनिहित वीणाम/वरदां संगीत मातृकां वंदे।
बायें स्तन पर वीणा टिकाये हुए संगीत की देवी की वंदना करते है। (खट्टर काका, पृष्ठ १६६)
स्मरेत् प्रथम पुष्पणीम्/रुधिर बिंदु नीलम्बराम्/घनस्तन भरोन्नताम्/त्रिपुर सुन्दरी माश्रये (खट्टर काका, पृष्ठ १६५)
‘प्रथम पुष्पिता होने के कारण जिनका वस्त्र रक्तरंजित हो गया है, वैसी पीनोन्नतस्तनी त्रिापुर सुन्दरी का आश्रय मैं ग्रहण करता हूँ।
कालतंत्र में काली का ध्यान-घोरदंष्ट्रा करालास्या पीनोन्नतपयोधरा/महाकालेन च समं विपरीतरतातुरा। (वही, पृष्ठ १६६)
कच कुचचिबुकाग्रे पाणिषु व्यापितेषु/प्रथम जलाधि-पुत्री-संगमेऽनंग धाग्नि/ग्रथित निविडनीवी ग्रन्थिनिर्मोंचनार्थं चतुरधिक कराशः पातु न श्चक्रमाणि। (वही, पृष्ठ १६७)
लक्ष्मी के साथ चतुर्भुज भगवान् का प्रथम संगम हो रहा है। उनके चारों हाथ फंसे हुए हैं। दो लक्ष्मी के स्तनों में, एक केश में, एक ठोढ़ी में। अब नीवी (साड़ी की गाँठ खोलें तो कैसे? इस काम के लिये एडीशनल हैंड (अतिरिक्त हाथ) चाहने वाले विष्णु भगवान् हम लोगों की रक्षा करें-पद्मायाः स्तनहेमसद्मनि मणिश्रेणी समाकर्षके/किंचित कंचुक-संधि-सन्निधिगते शौरेः करे तस्करे/सद्यो जागृहि जागृहीति बलयध्यानै र्ध्रुवं गर्जता/कामेन प्रतिबोधिताः प्रहरिकाः रोमांकुरः पान्तु नः।अर्थात् लक्ष्मी की कंचुकी में भगवान का हाथ घुस रहा है। यह देखकर कामदेव अपने प्रहरियों को जगा रहे हैं- उठो, उठो घर में चोर घुस रहा है। प्रहरी गण जागकर खड़े हो गये हैं। वे ही खड़े रोमांकुर हम लोगों की रक्षा करें। पार्वती की वंदना-गिरिजायाः स्तनौ वंदे भवभूति सिताननौ, तपस्वी कां गतोऽवस्थामिति स्मेराननाविव,….अंकनिलीनगजानन शंकाकुल बाहुलेयहृतवसनौ/समिस्तहरकरकलितौ हिमगिरितनयास्तनौ जयतः।(वही, पृष्ठ १६८)तो यह कामांध मस्तिष्क की वीभत्स परिणति जो देवी-देवताओं तक को नहीं छोड़ती लेकिन प्रचार किया जाता है कि देश की महान् संस्कृति स्त्रियों को पूज्य घोषित करती है
मूलचंद जी के लेख से कुछ आगे जारी रखते हुए …….
लेख के दूसरे भाग में वि.का. राजवाडे की पुस्तक ‘भारतीय विवाह संस्था का इतिहास’ के पृष्ठ १२८ से उद्धृत वाक्य को आपने देखा। इसी वाक्य के तारतम्य में ही आगे लिखा है, ‘‘यह नाटक होने के बाद रानी कहती है – महिलाओं, मुझसे कोई भी संभोग नहीं करता। अतएव यह घोड़ा मेरे पास सोता है।….घोड़ा मुझसे संभोग करता है, इसका कारण इतना ही है अन्य कोई भी मुझसे संभोग नहीं करता।….मुझसे कोई पुरुष संभोग नहीं कर रहा है इसलिए मैं घोड़े के पास जाती हूँ।” इस पर एक तीसरी कहती है – ‘‘तू यह अपना नसीब मान कि तुझे घोड़ा तो मिल गया। तेरी माँ को तो वह भी नहीं मिला।”
ऐसा है संभोग-इच्छा के संताप में जलती एक स्त्री का उद्गार, जिसे राज-पत्नी के मुँह से कहलवाया गया है। इसी पुस्तक के पृष्ठ १२६ पर अंकित यह वाक्य स्त्रियों की कामुक मनोदशा का कितना स्पष्ट विश्लेषण करता है, ‘‘बाद में प्रगति हासिल करके जब लोगों को अग्नि तैयार करने की प्रक्रिया का ज्ञान हुआ तब वे वन्य लोग अग्नि के आस-पास रतिक्रिया करते थे। किसी भी स्त्री को किसी भी पुरुष द्वारा रतिक्रिया के लिए पकड़कर ले जाना, उस काल में धर्म माना जाता था। यदि किसी स्त्री को, कोई पुरुष पकड़कर न ले जाए, तो वह स्त्री बहुत उदास होकर रोया करती थी कि उसे कोई पकड़कर नहीं ले जाता और रति सुख नहीं देता। इस प्रकार की स्त्री को पशु आदि प्राणियों से अभिगमन करने की स्वतंत्रता थी। वन्य ऋषि-पूर्वजों में स्त्री-पुरुष में समागम की ऐसी ही पद्धति रूढ़ थी।” यह कथन निर्विवाद रूप से स्त्रियों की उसी मानसिकता का उद्घाटन करता है कि वे संभोग के लिए न केवल प्रस्तुत रहती हैं, बल्कि उनका एकमात्र अभिप्रेत यौन-तृप्ति के लिए पुरुषों को प्रेरित करना है।
इस तरह के दृष्टांत वेद-पुराण इत्यादि में भी बहुततायत से उपलब्ध हैं। यहाँ ऋग्वेद के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं -
मेरे पास आकर मुझे अच्छी तरह स्पर्श करो। ऐसा मत समझना कि मैं कम रोयें वाली संभोग योग्य नहीं हूँ(यानी बालिग नहीं हूँ)। मैं गाँधारी भेड़ की तरह लोमपूर्णा (यानी गुप्तांगों पर घने रोंगटे वाली) तथा पूर्णावयवा अर्थात् पूर्ण (विकसित अधिक सटीक लगता है) अंगों वाली हूँ।(ऋ. १।१२६।७) (डॉ. तुलसीराम का लेख-बौद्ध धर्म तथा वर्ण-व्यवस्था-हँस, अगस्त २००४)
कोई भी स्त्री मेरे समान सौभाग्यशालिनी एवं उत्तम पुत्र वाली नहीं है। मेरे समान कोई भी स्त्री न तो पुरुष को अपना शरीर अर्पित करने वाली है और न संभोग के समय जाँघों को फैलाने वाली है।(ऋ. १०/८६/६) ऋग्वेद-डॉ. गंगा सहाय शर्मा, संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण १९८५)
हे इन्द्र! तीखे सींगों वाला बैल जिस प्रकार गर्जना करता हुआ गायों में रमण करता है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ रमण करो।(ऋ. १०/८६/१५) (वही)
ब्रह्म वैवर्त पुराण में मोहिनी नामक वेश्या का आख्यान है जो ब्रह्मा से संभोग की याचना करती है और ठुकराए जाने पर उन्हें धिक्कारते हुए कहती है, ‘‘उत्तम पुरुष वह है जो बिना कहे ही, नारी की इच्छा जान, उसे खींचकर संभोग कर ले। मध्यम पुरुष वह है जो नारी के कहने पर संभोग करे और जो बार-बार कामातुर नारी के उकसाने पर भी संभोग नहीं करे, वह पुरुष नहीं, नपुंसक है।(खट्टर काका, पृ. १८८, सं. छठाँ)
इतना कहने पर भी जब ब्रह्मा उत्तेजित नहीं हुए तो मोहिनी ने उन्हें अपूज्य होने का शाप दे दिया। शाप से घबराए हुए ब्रह्मा जब विष्णु भगवान से फ़रियाद करने पहुँचे तो उन्होंने डाँटते हुए नसीहत दिया, ‘‘यदि संयोगवश कोई कामातुर एकांत में आकर स्वयं उपस्थित हो जाए तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो कामार्त्ता स्त्री का ऐसा अपमान करता है, वह निश्चय ही अपराधी है। (खट्टर काका, पृष्ठ १८९) लक्ष्मी भी बरस पड़ीं, ‘‘जब वेश्या ने स्वयं मुँह खोलकर संभोग की याचना की तब ब्रह्मा ने क्यों नहीं उसकी इच्छा पूरी की? यह नारी का महान् अपमान हुआ।” ऐसा कहते हुए लक्ष्मी ने भी वेश्या के शाप की पुष्टि कर दी।(वही, पृष्ठ १८९)
विष्णु के कृष्णावतार के रूप में स्त्री-भोग का अटूट रिकार्ड स्थापित करके अपनी नसीहत को पूरा करके दिखा दिया। ब्रह्म वैवर्त में राधा-कृष्ण संभोग का जो वीभत्स दृश्य है उसका वर्णन डॉ. गंगासहाय ‘प्रेमी’ ने अपने लेख ‘कृष्ण और राधा’ में करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया इन शब्दों में व्यक्त किया है, ‘‘पता नहीं, राधा कृष्ण संभोग करते थे या लड़ाई लड़ते थे कि एक संभोग के बाद बेचारी राधा लहूलुहान हो जाती थी। उसके नितंब, स्तन और अधर बुरी तरह घायल हो जाते। राधा मरहम पट्टी का सामान साथ रखती होगी। राधा इतनी घायल होने पर प्रति रात कैसे संभोग कराती थी, इसे बेचारी वही जाने। (सरिता, मुक्ता रिप्रिंट भाग-२) इस प्रतिक्रिया में जो बात कहने को छूट गयी वह यह है कि इस हिंसक संभोग, जिसे बलात्कार कहना ज्यादा उचित है, से राधा प्रसन्न होती थी जिससे यही लगता है कि स्त्रियाँ बलात्कृत होना चाहती हैं।
History of prostitution in india के पृष्ठ १४७ पर पद्म पुराण के उद्धृत यह आख्यान प्रश्नगत प्रसंग में संदर्भित करने योग्य है। एक विधवा क्षत्राणी जो कि पूर्व रानी होती है, किसी वेद-पारंगत ब्राह्मण पर आसक्त होकर समर्पण करने के उद्देश्य से एकांत में उसके पास जाती है लेकिन ब्राह्मण इनकार कर देता है। इस पर विधवा यह सोचती है कि यदि वह उस ब्राह्मण के द्वारा बेहोशी का नाटक करे तो वह उसको ज+रूर अपनी बाँहों में उठा लेगा और तब वह उसे गले में हाथ डालकर और अपने अंगों को प्रदर्शित व स्पर्श कराकर उसे उत्तेजित कर देगी और अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगी। निम्न श्लोक उसकी सोच को उद्घाटित करते हैं – सुस्निग्ध रोम रहितं पक्वाश्वत्थदलाकृति।/दर्शयिष्यामितद्स्थानम् कामगेहो सुगन्धि च॥
मैं उसको पूर्ण विकसित पीपल के पत्ते की आकार की रोम रहित मृदुल और सुगंधित काम गेह(योनि) को (किसी न किसी तरह से) दिखा दूँगी क्योंकि – बाहूमूल कूचद्वंन्दू योनिस्पर्शन दर्शनात्।/कस्य न स्ख़लते चिन्तं रेतः स्कन्नच नो भवेत्॥
यह निश्चित है कि ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जिसका वीर्य किसी के बाहु-युगल, स्तन-द्वय और योनि को छूने और देखने से स्खलित न होता हो।
इससे ज्ञात होता है की आर्ष समाज से लेकर अर्वाचीन समाज तक स्त्रियों की छवि को एक विशेष खाँचे में फिट किया गया है, मातृ-सत्तात्मक समाज रहा हो या पितृ-सत्तात्मक स्त्री को देह की भाषा में ही व्यक्त करने और होने का खेल चलता रहा। और स्त्री को पूजा जाता है ये बकवास की जाती रही है ………………………..
परन्तु अब ये sambhav nahi reh gaya है
मूलचन्द सोनकर ji ke lekh ke ansh
पा.ना. सुब्रमणियन द्वारा लिखा एक लेख है जिसके कुछ अंश इस दिशा में सहायक सिद्ध होंगे की नारी का कितना सम्मान किया जाता रहा है ………………..
कदम्ब वंशीय राजा मयूर शर्मन के समय सर्वप्रथम केरल में ब्राह्मणों का आगमन हुआ. उसके पहले वहां बौद्ध एवं जैन धर्म का बोलबाला रहा. कुछ ब्राह्मण पंडितों ने शास्त्रार्थ कर वहां के बौद्ध भिक्षुओं को परास्त कर दिया. शंकराचार्य (७८८-८२०) के नेतृत्व में हिंदू/सनातन धर्म के पुनरूत्थान के प्रयास स्वरुप शनै शनै बौद्ध तथा जैन धर्म के अनुयायी कम होते चले गए. चेर वंश के कुलशेखर राजाओं (८०० – ११००) ने भी ब्राह्मणों को प्राश्रय और प्रोत्साहन दिया. कहते हैं कि जो ब्राह्मण उत्तर दिशा से आए उन्हें केरल के ३२ और कर्णाटक के तुलुनाडु के ३२ गांवों में बसाया गया था. यही वहां के नम्बूतिरी ब्राह्मण कहलाते हैं जो अपने आपको स्थानीय कहते हैं. कालांतर में इन्हीं ब्राह्मणों में उपलब्ध भूमि आबंटित कर दी गई थी और एक तरह से वे ही वहां के जमींदार बन बैठे. वे जमीन पट्टे पर दूसरों को खेती या अन्य प्रयोजन के लिए दे दिया करते और एवज में उन्हें वार्षिक भू राजस्व की प्राप्ति होती थी. (कृषि उत्पाद या तरल मुद्रा के रूप में)
नम्बूतिरी ब्राह्मणों के निवास को “मना” और कुछ जगह “इल्लम” कह कर पुकारते है. ये साधारणतया एक बड़े भूभाग पर आलीशान बने होते हैं. इसी के अन्दर सेवकों आदि के निवास की भी व्यवस्था होती थी. नाम्पूतिरी लोग भी उत्तर भारतीय पंडितों की तरह चुटैय्या धारण करते थे लेकिन इनकी चोटी पीछे न होकर माथे के ऊपर कोने में हुआ करती थी. इष्ट देव की आराधना में मन्त्र के अतिरिक्त तंत्र की प्रधानता होती है. पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी केवल ज्येष्ठ पुत्र ही हुआ करता था और वही एक मात्र व्यक्ति विवाह करने का भी अधिकारी होता था. पत्नियों की संख्या चार तक हो सकती थी (Polygamy). परिवार के सभी सदस्य एक साथ “मना” में ही निवास करते थे. इस व्यवस्था से संपत्ति विघटित न होकर यथावत बनी रहती थी. अब परिवार के जो दूसरे युवा हैं उन्हें इस बात की स्वतंत्रता दी गई थी कि वे चाहें तो बाहर किसी अन्य ज़ाति (क्षत्रिय अथवा शूद्र) की महिलाओं, अधिकतम चार से “सम्बन्ध” बना सकते थे. ऐसे सम्बन्ध अधिकतर अस्थायी ही होते थे. “सम्बन्ध” बनने के लिए पसंदीदा स्त्री को भेंट स्वरुप वस्त्र (केवल एक गमछे से काम चल जाता था) दिए जाने की परम्परा थी. वस्त्र स्वीकार करना “सम्बन्ध” की स्वीकारोक्ति हो जाया करती थी. जिस महिला से “सम्बन्ध” बनता था, उसके घर रहने के लिए रात में जाया करते और सुबह उठते ही वापस अपने घर “मना” आ जाते. रात अंधेरे में सम्बन्धम के लिए जाते समय अपने साथ एक लटकने वाला दीप भी ले जाते, जिसकी बनावट अलग प्रकार की होती थी और इसे “सम्बन्धम विलक्कू” के नाम से जाना जाता था.
नम्बूतिरी ब्राह्मणों की इस सामाजिक व्यवस्था के परिणाम स्वरुप जहाँ उनकी आबादी कम होती चली गई, वहीं दूसरी तरफ़ योग्य वर के न मिल पाने के कारण कई नम्बूतिरी कन्यायें अविवाहित ही रह जाती. अंततोगत्वा भारत में हिन्दुओं के लिए समान/सार्वजनिक विवाह और उत्तराधिकार नियम बन जाने से उनकी रुढिवादी परम्पराओं का अंत हुआ. केरल में १९६५-७० में भूमि सुधार कानूनों के लागू होने से नम्बूतिरी घरानों की सम्पन्नता भी जाती रही.
केरल के समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग नायरों (इसमे पिल्लई, मेनोन, पणिक्कर, मारार, नम्बियार, कुरूप आदि लोग भी शामिल हैं) का था. तकनीकी दृष्टि से ये शूद्र थे परन्तु योद्धा हुआ करते थे. सेना में ये कार्यरत होते थे अतः क्षत्रिय सदृश माना जा सकता है. इनके समाज में अधिकार स्त्रियों के हाथों हुआ करता था. उत्तराधिकार के नियम आदि स्त्रियों पर केंद्रित थे. इस व्यवस्था को “मरुमक्कतायम” कहा जाता था. इन लोगों में विवाह नामकी कोई संस्था नहीं थी. घर की लड़कियां अपने अपने घरों (जिन्हें “तरवाड़” कहा जाता है) में ही रहतीं. सभी भाई बहन इकट्ठे अपनी माँ के साथ. घर के मुखिया के रूप में मामा(मुजुर्ग महिला का भाई) नाम के लिए प्रतिनिधित्व करता था. किसी कन्या के रजस्वला होने पर किसी उपयुक्त पुरूष की तलाश होती जिस के साथ “सम्बन्धम” किया जा सके. यहीं नम्बूतिरी ब्राहमणों का काम बन जाता था क्योंकि कई विवाह से वंचित युवक किसी सुंदर कन्या से संसर्ग के लिए लालायित रहते थे . नायर परिवार में “सम्बन्धम” के लिए नम्बूतिरी या अन्य ब्राह्मण पहली पसंद होती थी क्योंकि उन्हें बुद्धिमान समझा जाता था. जैसे नम्बूतिरी घरों के युवकों को चार स्त्रियों से सम्बन्धम की अनुमति थी वैसे ही यहाँ नायर समुदाय की स्त्रियों के लिए भी आवश्यक नहीं था कि वे केवल एक से ही सम्बन्ध बनाये रखें. एक से अधिक (Polyandry) भी हो सकते थे. अंशकालिक!. सम्बन्धम, जैसा पूर्व में ही कहा जा चुका है, साधारणतया अस्थायी पाया गया है. लेकिन स्थायी सम्बन्धम भी होते थे, किसी दूसरे संपन्न तरवाड़ के नायर युवक से. कभी कभी एक स्थाई और कुछ दूसरे अस्थायी/ अंशकालिक. एक से अधिक पुरुषों से सम्बन्ध होने की स्थिति में समय का बटवारा भी होता था. पुरूष रात्रि विश्राम के लिए स्त्री के घर आता और सुबह उठते ही अपने घर चला जाता. संतानोत्पत्ति के बाद बच्चों की परवरिश का कोई उत्तरदायित्व पुरूष का नहीं रहता था. सब “तरवाड़” के जिम्मे. परिवार की कन्याओं का सम्बन्ध धनी नम्पुतिरियों से रहने के कारण धन “मना” से “तरवाड़” की और प्रवाहित होने लगा और “तरवाड़” धनी होकर प्रतिष्ठित हो गए. कुछ तरवाडों की प्रतिष्ठा इतनी रही कि वहां की कन्याओं से सम्बन्ध बनना सामाजिक प्रतिष्ठा का भी द्योतक रहा.
नायरों जैसी ही स्थिति राज परिवारों की भी रही. उनकी कन्याओं का सम्बन्ध किसी दूसरे राज परिवार के पुरूष या किसी ब्राह्मण से हो सकता था और राज परिवार के युवकों का सम्बन्ध नायर परिवार की कन्याओं के साथ.
यहाँ यह बताना उचित होगा कि इस पूरी व्यवस्था को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी और किसी भी दृष्टिकोण से इसे हेय नहीं समझा जाता था.
‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ के द्वारा स्मृतिकार कहीं से भी यह नहीं कहना चाहता कि स्त्री पूज्यनीय है। यदि बहुप्रचारित (यद्यपि दुष्प्रचारित कहना ज्यादा सटीक है) अर्थ ही लिया जाए तो भी यह सिद्ध नहीं होता कि स्त्रियों के बारे में इससे भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व रेखांकित होता है। यह श्लोक हाईपोथीसिस की बात करता है किसी प्रकार का आदेश नहीं देता। ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी ने इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया है, ‘‘जिस कुल में स्त्रियाँ पूजित (सम्मानित) होती हैं, उस कुल से देवता प्रसन्न होते हैं।” इस अनुवाद से भी यही सिद्ध होता है कि यह एक अन्योन्याश्रित स्थिति है अर्थात् स्त्रियों को पूज्य घोषित करने का कोई बाध्यकारी आदेश नहीं दिया। मनु ने, जैसा कि उन्हें प्रताड़ित अपमानित करने के लिए आदेशित किया है। यही कारण है कि स्त्रियों के बारे में पुरुषों में अच्छी धारणा अंकुरित ही नहीं हो पायी।
मनुस्मृति ने स्त्रियों की अस्मिता और स्वाभिमान पर कितने तरीक़े से हमला किया है, उसकी बानगी देखिये-शूद्र की शूद्रा ही पत्नी होती है। वैश्य को वैश्य और शूद्र दोनों वर्ण की कन्यायों से, क्षत्रिय को क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों वर्ण की कन्याओं से तथा ब्राह्मण को चारों वर्णों की कन्याओं से विवाह करने का अधिकार है। (३.१३)
लेकिन इसके तुरन्त बाद वाला श्लोक आदेश देता है-ब्राह्मण और क्षत्रिय को स्वर्णा स्त्री न मिलने पर भी शूद्रा को स्त्री बनाने का किसी भी इतिहास में आदेश नहीं पाया जाता। (३.१४)
इसके आगे के श्लोकों में भी शूद्र वर्ण की स्त्री के लिये तमाम घिनौनी बातें कही गई हैं लेकिन निम्न श्लोक में तो सारी सीमाओं को तोड़कर रख दिया- जो शूद्रा के अधर रस का पान करता है उसके निःश्वास से अपने प्राण-वायु को दूषित करता है और जो उनमें सन्तान उत्पन्न करता है उसके निस्तार का कोई उपाय नहीं है। (३.१९)
किन्तु जैसे ही याद आया कि इससे स्त्रियों को अबाध भोगने के अधिकार से सवर्ण पुरुष वंचित हो जायेंगे तो कह दिय-स्त्रियों का मुख सदा शुद्ध होता है….(५.१३०)
अब स्त्रियों पर कुछ सामान्य टिप्पणियाँ भी देखिये-
मदिरा पीना, दुष्टों की संगति, पति का वियोग, इधर-उधर घूमना, कुसमय में सोना और दूसरों के घरों में रहना ये छः स्त्रियों के दोष है। (२.१३)
स्त्रियाँ रूप की परीक्षा नहीं करतीं, न तो अवस्था का ध्यान रखती हैं, सुन्दर हो या कुरूप हों, पुरुष होने से ही वे उसके साथ संभोग करती हैं। (९.१४)
पुंश्चल (पराये पुरुष से भोग की इच्छा) दोष से, चंचलता से और स्वभाव से ही स्नेह न होने के कारण घर में यत्नपूर्वक रखने पर भी स्त्रियाँ पति के विरुद्ध काम करती हैं। (९.१५)
ब्रह्मा जी ने स्वभाव से ही स्त्रियों का ऐसा स्वभाव बनाया है, इसलिये पुरुष को हमेशा स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। (९.१६)
मनु जी ने सृष्ट्यादि में शय्या, आसन, आभूषण, काम, क्रोध, कुटिलता, द्रोह और दुराचार स्त्रियों के लिए ही कल्पना की थी। (९.१७)
ऐसे न जाने कितने श्लोक पूरी मनु स्मृति में फैले पड़े हैं।
ऋग्वेद के मंत्र १०।८५।३७ हो या मनु स्मृति के नवें अध्याय के श्लोक ३३ से लेकर ५२ तक स्त्रियों को पुरुषों की खेती कहा गया है। इस्लाम भी कुरान की आयत १.२.१२३ के द्वारा इसी प्रकार की व्यवस्था करता है
ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी (सुं.कां. ६२-३) का उद्घोष करने वाले तुलसीदास ने भी स्त्री-निंदा में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ा। ‘सरिता’ फरवरी १९५६(सरिता मुक्ता रिप्रिंट भाग-१) के अंक में ‘रामचरितमानस में नारी’ शीर्षक से प्रकाशित लेख में इसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। ऐसा करने में उन्होंने भी मनु की शूद्र स्त्री को अलग खाने में रखा है। संदर्भित लेख से ही कुछ उद्धरणों को देकर इसे स्पष्ट किया जा रहा है- करै विचार कुबुद्धि कुजाती। होई अकाजु कवनि विधि राती।/देखि लागि मधु कुटिल किराती। जिमि गंव तकै लेऊँ केहि भाँति॥/भरत मातु पहि गइ बिलखानी। का अनमनि हसि कह हँसि रानी॥/उतरू देहि नहिं लेइ उसासू। नारि चरित करि ढारइ आँसू।
खोटी बुद्धि वाली और खोटी-नीच जाति वाली मंथरा विचार करने लगी कि रात ही रात में यह काम कैसे बिगाड़ा जाए? जिस तरह कुटिल भीलनी शहद के छत्ते को लगा देखकर अपना मौका ताकती है कि इसको किस तरह लूँ। वह बिलखती हुई भरत की माता कैकेई के पास गई। उसको देखकर कैकेई ने कहा कि आज तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ जवाब नहीं देती और लंबी साँस खींचती है और स्त्री चरित्रकरके आँखों से पानी टपकाती है।
मंथरा कैकेई के लिए ही मरती रहती है लेकिन तुलसीदास ने कैकेई के ही मुँह से उसके लिए यह कहलवाया – काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। तिय विसेखि मुनि चेरि कहि भरत मातु मुसकानि।
काने, लंगड़े, लूले – ये बड़े कुटिल और कुचाली होते हैं और उनमें भी स्त्री और विशेष रूप से दासी-ऐसा कहके भरत मातु मुसकाई।
इतने विशेषणों से उसे तब अलंकृत किया गया जबकि स्वयं सरस्वती ने उसकी मति फेरी थी, अर्थात् सरस्वती भी स्त्री होने के कारण लपेटे में। सीता और पार्वती को भी क्रमशः राम और शिव की किंकरी ही घोषित कराया है। तुलसीदास ने और वह भी उनकी माता के ही मुँह से। सीता की माँ सीता की विदाई के समय राम से कहती है – तुलसी सुसील सनेहु लखि निज किंकरी कर मानिबी।
इसके सुशील स्वभाव और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी मानियेगा। बिल्कुल यही बात पार्वती की माँ भी बेटी को विदा करते समय शिव से कहती है – नाथ उमा मम प्रान सम गृह किंकरी करेहु/छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु।
हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान है। अब इसे अपने घर की दासी बनाइये और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए-करेहु सदा संकर पद पूजा। नारि धरम पति देव न दूजा॥
पार्वती को उपदेश देते हुए कहती हैं कि हे पुत्री, तू सदा शिव के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जब ईश्वर या उसके अवतार द्वारा स्वयं ही पत्नी को अपने चरण में जगह दी जाती है तो पुरुष क्यों नहीं करेगा अथवा उसे क्यों नहीं करना चाहिए?
गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित रामचरित मानस के एक सौ छठवें संस्करण में निम्न दृष्टांत उद्धृत किए जा रहे हैं – माता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी॥/होई विकल सक मनहि न रोकी। जिमि रबि मनि द्रव रबिहि विलोकी॥ (पृष्ठ ६२६)
स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि ‘सूर्य’ को देखकर द्रवित हो जाती है।
सती अनसूया द्वारा सीता को उपदेश देते समय उनके मुँह से स्त्रियों के बारे में जो कहलवाया गया है, वह पृष्ठ संख्या ६०९ और ६१० पर अंकित है। देखिए – धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काल परिखिअहिं चारी॥/वृद्ध रोग सब जड़ धन हीना।/ अंध बधिर क्रोधी अति दीना॥/ऐसेहु पति कर किएँ अपमाना।/नारि पाव जमपुर दुखनाना॥/एकइ धर्म एक व्रत नेमा।/कायॅ वचन मन पति पद प्रेमा॥
धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री – इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यन्त ही दीन-ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भाँति-भाँति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए, बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है-जग पतिव्रता चारि विधि अहहीं। वेद पुरान संत सब कहहीं॥/उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं॥
जगत् में चार प्रकार की पतिव्रताएँ हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत् में(मेरे पति को छोड़कर) दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है-मध्यम परपति देखइ कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे॥/धर्म विचारी समुझि कुल रहईं।/सा निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहईं॥
मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो(अर्थात् समान अवस्था वाले वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है।) जो धर्म के विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं- बिन अवसर भय तें रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई॥/पति बंचक परपति रति करई। रौरव नरक कल्प सत परई॥
जो स्त्री मौका न मिलने से या भयावश पतिव्रता बनी रहती है, जगत् में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो सौ कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है-छन सुख लागि जनम सत कोटी। दुख न समुझ तेहि सम को खोटी॥/बिनु श्रम नारि परम गति लहई। पतिब्रत धर्म छाड़ि छल गहई॥
क्षणभर के सुख के लिए जो सौ करोड़ (असंख्य) जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है – पति पतिकूल जनम जहँ जाई। बिधवा होइ पाइ तरुनाई॥
किन्तु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर (भरी जवानी में) विधवा हो जाती है – सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ।/जसु गावति श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिंहि प्रिय॥
स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किन्तु पति की सेवा करके यह अनायास ही शुभगति प्राप्त कर लेती है। (पतिव्रत धर्म के कारण) आज भी ‘तुलसी जी’ भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं।
तुलसीदास जी को पुरुषों में कोई दोष नहीं दिखाई देता तो इसके पीछे पुरुष की वही स्त्री विरोधी मानसिकता है जिसे बड़े करीने से धर्मशास्त्र की सान पर परवान चढ़ाकर विकसित किया गया है और जो आज भी क़ायम है।
(मूलचंद जी के लेख से …….)
कबीर तुलसी के समकालीन माने जाते हैं : परन्तु दोनों का रचना-संसार समान नहीं है। आज कबीर को सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, शोषितों, पीड़ितों के प्रबल पक्षकार के रूप में देखा जाता है लेकिन स्त्रियों की निंदा करने में वह भी किसी से पीछे नहीं है। डॉ. युगेश्वर द्वारा सम्पादित और हिन्दी प्रचारक संस्थान वाराणसी द्वारा प्रकाशित ‘कबीर समग्र’ के प्रथम संस्करण १९९४ से कुछ साखियाँ यहाँ उद्धृत की जा रही हैं :-
कामणि काली नागणीं तीन्यूँ लोक मंझारि।
राम सनेही ऊबरे, विषई खाये झारि॥
(पृष्ठ २८४)
एक कनक अरु कॉमिनी, विष फल कीएउ पाइ।
देखै ही थै विष चढै+, खॉयै सूँ मरि जाइ॥
(पृष्ठ २८६)
नारी कुंड नरक का, बिरला थंभै बाग।
कोई साधू जन ऊबरै, सब जग मूँवा लाग॥
(पृष्ठ २८६)
जोरू जूठणि जगत की, भले बुरे का बीच।
उत्थम ते अलग रहैं, निकट रहें तें नीच॥
(पृष्ठ २८६)
सुंदरि थै सूली भली, बिरला बंचै कोय।
लोह निहाला अगनि मैं, जलि बलि कोइला होय॥
(पृष्ठ २८६)
इक नारी इक नागिनी, अपना जाया खाय।
कबहूँ सरपटि नीकसे, उपजै नाग बलाय॥
(पृष्ठ ४३७)
सर्व सोनाकी सुन्दरी, आवै बास सुबास।
जो जननी ह्नै आपनी, तौहु न बैठे पास॥
(पृष्ठ ४३७)
गाय भैंस घोड़ी गधी, नारी नाम है तास।
जा मंदिर में ये बसें, तहाँ न कीजै बास॥
(पृष्ठ ४३८)
छोटी मोटी कामिनी, सब ही विष की बेल।
बैरी सारे दाब दै, यह मारै हँसि खेल॥
(पृष्ठ ४४०)
नागिन के तो दोय फन, नारी के फन बीस।
जाको डस्यो न फिरि जिये, मरि है बिस्वा बीस॥
(पृष्ठ ४४०)
इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्री निंदा में कोई किसी से कम नहीं है।
आर्ष समाज से लेकर अर्वाचीन समाज तक स्त्रियों की छवि को एक विशेष खाँचे में फिट किया गया है, मातृ-सत्तात्मक समाज रहा हो या पितृ-सत्तात्मक स्त्री को देह की भाषा में ही व्यक्त करने और होने का खेल चलता रहा। इस खेल में स्त्री भी बराबर की हिस्सेदार रही। उसने इस आरोपण को सच की तरह अंगीकृत कर लिया कि वह एक देह है और इस देह की एक मात्र आवश्यकता है यौन-तृप्ति। यह मानते हुए भी कि यौन-सम्बन्ध द्विपक्षीय अवधारणा है जिसके प्रति पुरुष भी उतना ही लालायित रहता है। विकास के किसी भी मोड़ पर पुरुषों की काम-प्रवृत्ति का उस तरह से मनोविश्लेषण नहीं किया गया जैसा कि स्त्रियों का। इसका परिणाम यह हुआ कि सारी वर्जनाएँ स्त्रियों पर ही थोप दी गईं और पुरुषों को स्वच्छंद छोड़ दिया गया और वे स्त्रियों के साथ निर्द्वन्द्व होकर मनमानी करते रहे। स्त्रियाँ भोग्या बनने और वर्जनाओं के उल्लंघन के नाम पर लांछित होने को अभिशप्त होती रहीं। यही उनकी नियति बन गयी और उन्हीं के मुँह से इसे स्वीकार भी कराया गया। यह पुरुष-सत्तात्मक समाज के नीति-नियामकों की जीत और स्त्रियों की सबसे बड़ी हार थी, जिस पर ईश्वर की सहमति का ठप्पा भी लगवा लिया गया।
वेद, पुराण और महाभारत से उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार इन ग्रन्थों में स्त्रियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है। वेदों में वर्णित कुछ कामुक दृष्टांत हरिमोहन झा की पुस्तक ‘खट्टर काका’ से साभार लेकर यहाँ पर उद्धृत किए जा रहे हैं – मर्य इव युवतिभिः समर्षति सोमः/कलशे शतयाम्ना पथा (ऋ. ९/८६/१६)
कलश में अनेक धारों से रस का फुहारा छूट रहा है। जैसे, युवतियों में… (पृष्ठ १९४)
को वा शयुत्र विधवेव देवरं मर्यं न योषा वृणुते (ऋ. ७/४०/२)
‘‘जैसे विधवा स्त्री शयनकाल में अपने देवर को बुला लेती है, उसी प्रकार मैं भी यज्ञ में आपको सादर बुला रही हूँ। (पृष्ठ १९५)
यत्र द्वाविव जघनाधिषवरण्या/उलूखल सुतानामवेद्विन्दुजल्गुलः (ऋ. १/२८/२)
‘‘जैसे कोई विवृत-जघना युवती अपनी दोनों जंघाओं को फैलाये हुई हो और उसमें..(पृष्ठ १९३)
अभित्वा योषणो दश, जारं न कन्यानूषत/मृज्यसे सोम सातये (ऋ. ९/५६/३)
‘‘कामातुरा कन्या अपने जार (यार ) को बुलाने के लिये इसी प्रकार अंगुलियों से इशारा करती हैं। (पृष्ठ १९३ )
वृषभो न तिग्मश्रृंगोऽन्तर्यूथेषु रोरुवत्! (ऋ. १०/८६/१५)
अर्थात् ‘जिस प्रकार टेढ़ी सींग वाला साँड़ मस्त होकर डकरता हुआ रमण करता है, उसी प्रकार तुम भी मुझसे करो। (पृष्ठ १९६)
डॉ. तुलसीराम ने अपने लेख ‘बौद्ध धर्म तथा वर्ण व्यवस्था’ (‘हंस’, अगस्त २००४) में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के छठवें मंत्र का अनुवाद इस तरह किया है, ‘‘यह संभोग्य युवती (यानी जिसके गुप्तांग पर बाल उग आए हों) अच्छी तरह आलिंगन (बद्ध) होकर सूतवत्सा नकुली (यानी एक रथ हाँकने वाले की बेटी, जिसका नाम नकुली था) की तरह लम्बे समय तक रमण करती है। वह बहु-वीर्य सम्पन्न युवती मुझे अनेक बार भोग प्रदान करती हैं।” इसी लेख में यह भी कहा गया है कि ऋग्वेद के अंग्रेजी अनुवाद राल्फ टी ग्रीफिथ को दसवें मंडल के ८६ वें सूक्त के मंत्र १६ और १७ इतने वीभत्स लगे कि उन्होंने इनका अनुवाद ही नहीं किया।
ऋग्वेद के दसवें मंडल के दसवें सूक्त में सहोदर भाई-बहन यम और यमी का संवाद है जिसमें यमी यम से संभोग याचना करती है। इसी मंडल के ६१ वें सूक्त के पाँचवें-सातवें तथा अथर्ववेद (९/१०/१२) में प्रजापति का अपनी पुत्री के साथ संभोग वर्णन है। यम और यमी के प्रकरण का विवरण अथर्ववेद के अठारहवें कांड में भी मिलता है। (भारतीय विवाह संस्था का इतिहास – वि.का. राजवाडे, पृष्ठ ९७) इसी पुस्तक के पृष्ठ ७८-७९ पर पिता-पुत्री के सम्बन्धों पर चर्चा करते हुए वशिष्ठ प्रजापति की कन्या शतरूपा, मनु की कन्या इला, जन्हू की कन्या जान्हवी (गंगा) सूर्य की पुत्राी उषा अथवा सरण्यू का अपने-अपने पिता के साथ पत्नी भाव से समागन होना बताया गया है। ‘स्त्री-पुरुष समागम सम्बन्धी कई अति प्राचीन आर्ष प्रथाएँ नामक यह अध्याय सगे-सम्बन्धियों के मध्य संभोग-चर्चा पर आधारित है। इस प्रकार के सम्बन्धों की चर्चा महाभारत के ‘शांतिपूर्व’ के २०७ वें अध्याय के श्लोक संख्या ३८ से ४८ तक में भीष्म द्वारा की गई है। राजवाडे ने अपनी उक्त संदर्भित पुस्तक के पृष्ठ ११५-११६ पर (श्लोक का क्रम ३७ से ३९ अंकित है।) इन श्लोकों का अर्थ निम्नवत् किया है- कृतयुग (संभवतः सतयुग) में स्त्री-पुरुषों के बीच, जब मन हुआ तब, समागम हो जाता था। माँ, पिता, भाई, बहन का भेद नहीं था। वह यूथावस्था थी। (श्लोक सं. ३८) त्रेता युग में स्त्री-पुरुषों द्वारा एक-दूसरे को स्पर्श करने पर समाज उन्हें उस समय के लिए संभोग करने की अनुमति देता था। यह पसन्द-नापसन्द या प्रिय-अप्रिय का चुनाव करने की व्यवस्था थी। (श्लोक सं. ३९) द्वापर युग में मैथुन धर्म शुरू हुआ। इस पद्धति के अनुसार, स्त्री-पुरुष अपनी टोली में जोड़ियों में रहने लगे, किन्तु अभी भी इन जोड़ियों को स्थिर अवस्था प्राप्त नहीं हुई थी और कलियुग में द्वंद्वावस्था की परिणति हुई, अर्थात् जिसे हम विवाह संस्था कहते हैं उसका उदय हुआ। (श्लोक सं. ४०)
‘खट्टर काका’ के पृष्ठ ६४ पर भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग खंड के हवाले से उद्धृत निम्न श्लोक की मानें तो ईश्वरीय सत्ता के तीनों शीर्ष प्रतीक भी इस स्वच्छन्द सम्बन्ध से मुक्त नहीं हैं-स्वकीयां च सुतां ब्रह्मा विष्णुदेवः स्वमातरम्/भगनीं भगवान् शंभुः गृहीत्वा श्रेष्ठतामगात्!
स्त्री के मुँह से ही स्त्रियों की बुराई सिद्ध करने के आख्यान मिलते हैं। स्त्रियों का यह चरित्र- चित्राण उनकी विश्व-विख्यात ईर्ष्या-भावना की छवि को उद्घाटित करता है। इस प्रकार का एक दृष्टांत महाभारत से यहाँ पर उद्धृत है। आगे, सम्बन्धित खंड में रामरचितमानस से भी ऐसा ही दृष्टांत उद्धृत किया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अन्तर्गत ‘दानधर्म’ पर्व में पंचचूड़ा, अप्सरा और नारद के मध्य एक लम्बा संवाद है, जिसमें पंचचूड़ा स्त्रियों के दोष गिनती है। इसमें से कुछ श्लोकार्थ यहाँ दिये जा रहे हैं-नारद जी! कुलीन, रूपवती और सनाथ युवतियाँ भी मर्यादा के भीतर नहीं रहतीं। यह स्त्रियों का दोष है॥११॥ प्रभो! हम स्त्रियों में यह सबसे बड़ा पातक है कि हम पापी पुरुषों को भी लाज छोड़कर स्वीकार कर लेती हैं॥१४॥ इनके लिये कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है, जो अगम्य हो। इनका किसी अवस्था-विशेष पर भी निश्चय नहीं रहता। कोई रूपवान हो या कुरूप; पुरुष है- इतना ही समझकर स्त्रियाँ उसका उपभोग करती हैं॥१७॥ जो बहुत सम्मानित और पति की प्यारी स्त्रियाँ हैं; जिनकी सदा अच्छी तरह रखवाली की जाती है, वे भी घर में आने-जाने वाले कुबड़ों, अन्धों, गूँगों और बौनों के साथ भी फँस जाती है॥२०॥ महामुनि देवर्षे! जो पंगु हैं अथवा जो अत्यन्त घृणित मनुष्य (पुरुष) हैं, उनमें भी स्त्रियों की आसक्ति हो जाती है। इस संसार में कोई भी पुरुष स्त्रियों के लिये अगम्य नहीं हैं॥२१॥ ब्रह्मन! यदि स्त्रियों को पुरुष की प्राप्ति किसी प्रकार भी सम्भव न हो और पति भी दूर गये हों तो वे आपस में ही कृत्रिम उपायों से ही मैथुन में प्रवृत्त हो जाती हैं॥२२॥ देवर्षे! सम्पूर्ण रमणियों के सम्बन्ध में दूसरी भी रहस्य की बात यह है कि मनोरम पुरुष को देखते ही स्त्री की योनि गीली हो जाती है॥२६॥ यमराज, वायु, मृत्यू, पाताल, बड़वानल, छुरे की धार, विष, सर्प और अग्नि – ये सब विनाश हेतु एक तरफ और स्त्रियाँ अकेली एक तरफ बराबर हैं॥२९॥ नारद! जहाँ से पाँचों महाभूत उत्पन्न हुए हैं, जहाँ से विधाता ने सम्पूर्ण लोकों की सृष्टि की है तथा जहाँ से पुरुषों और स्त्रियों का निर्माण हुआ है, वही से स्त्रियों में ये दोष भी रचे गये हैं (अर्थात् ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं।)॥३०॥
इस आख्यान से दो बातें स्पष्ट सिद्ध होती है। पहली एक ही स्रोत से रची गई चीजों में विधाता ने मात्र स्त्रियों के लिये ही दोषों की रचना करके पक्षपात किया और दूसरी यह कि स्वयं विधाता ही पुरुष-वर्चस्व का पोषक है।
मूलचंद जी के लेख से आगे जारी रखते हुए …….
हमारे शास्त्र कन्या-संभोग और बलात्कार के लिये भी प्रेरित करते हैं। मनुस्मृति के अध्याय ९ के श्लोक ९४ में आठ वर्ष की कन्या के साथ चौबीस वर्ष के पुरुष के विवाह का प्रावधान है। ‘भारतीय विवाह का इतिहास’(वि.का. राजवाडे) के पृष्ठ ९१ पर उद्धृत वाक्य ‘‘चौबीस वर्ष का पुरुष, आठ वर्ष की लड़की से विवाह करे, इस अर्थ में स्मृति प्रसिद्ध है। विवाह की रात्रिा में समागम किया जाय, इस प्रकार के भी स्मृति वचन हैं। अतः आठ वर्ष की लड़कियाँ समागमेय हैं, यह मानने की रूढ़ि इस देश में थी, इसमें शक नहीं।” इसी पुस्तक के पृष्ठ ८६-८७ तथा ९० के नीचे से चार पंक्तियों को पढ़ा जाय तो ज्ञात होता है कि कन्या के जन्म से लेकर छः वर्ष तक दो-दो वर्ष की अवधि के लिये उस पर किसी न किसी देवता का अधिकार होता था। अतः उसके विवाह की आयु का निर्धारण आठ वर्ष किया गया। क्या इससे यह संदेश नहीं जाता कि कन्या जन्म से ही समागमेय समझी जाती थी क्योंकि छः वर्ष बाद उस पर से देवताओं का अधिकार समाप्त हो जाता था। यम संहिता और पराशर स्मृति दोनों ही रजस्वला होने से पूर्व कन्या के विवाह की आज्ञा देते हैं (खट्टर काका पृष्ठ १०१) निम्न श्लोक देखें-प्राप्ते तु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति/मासि मासि रजस्तयाः पिब्रन्ति पितरोऽनिशम्। (यम संहिता)
यदि कन्या का विवाह नहीं होता और यह बारह वर्ष की होकर रजस्वला हो जाती है तो उसके पितरों को हर माह रज पीना पड़ेगा-रोमकाले तु संप्राप्ते सोमो सुंजीथ कन्यकाम/रजः काले तुः गंधर्वो वद्दिस्तु कुचदर्शने।
रोम देखकर सोम देवता, पुष्प देखकर गंधर्व देवता और कुच देखकर अग्नि देवता कन्या का भोग लगाने पहुँच जायेंगे।
जिस धर्म के देवता इतने बलात्कारी, उस धर्म के अनुयायी तो उनका अनुसरण करेंगे ही। कुंती के साथ सूर्य के समागम का विवरण राजवाडे के शब्दों में इस प्रकार है,-’वनपर्व’ के ३०७वें अध्याय में सूर्य कहता है- ‘‘हे कुंती, कन्या शब्द की उत्पत्ति, कम् धातु से हुई और इसका अर्थ है- चाहे जिस पुरुष की इच्छा कर सकने वाली। कन्या स्वतंत्र है, स्त्रियों और पुरुषों में किसी प्रकार का परदा या मर्यादा न होना- यही लोगों की स्वाभाविक स्थिति है, विवाहादि संस्कार सब कृत्रिम हैं, अतः तुम मेरे साथ समागम करो, समागम करने के बाद तुम पुनरपि कुमारी ही, अर्थात् अक्षत योनि ही रहोगी।” (वही, पृष्ठ ८९-९०) और देवराज इन्द्र द्वार बलात्कार के किस्से तो थोक के भाव मौजूद है।
यह रहा, तथाकथित पूज्य वेदों, पुराणों, महाभारत इत्यादि का स्त्रियों के प्रति रवैये की छोटी-सी बानगी। संस्कृत वाङ्मय के ग्रन्थ अथवा साहित्यिक रचनायें अथवा उनसे प्रेरित श्रृंगारिक कवियों की श्रृंगारिक भाषायी रचनाओं से लेकर आधुनिकता का लिबास ओढ़े चोली के पीछे क्या है…. ‘अथवा’ मैं चीज बड़ी हूँ मस्त-मस्त….. तक के उद्घोष में स्त्री-पुरुष बराबर के साझीदार हैं। इन कृतियों में से होकर एक भी रास्ता ऐसा नहीं जाता जिस पर चलकर स्त्री सकुशल निकल जाये, फिर भी वह इनके प्रति सशंकित नहीं है तो इस पर गहन, गम्भीर विमर्श होना चाहिये। सबसे बड़ी विडम्बना तो स्त्रियों का कृष्ण के प्रति अनुराग है जबकि स्त्रियों के साथ कृष्ण-लीला इनके चरित्र का सबसे कमजोर पहलू है। ब्रह्म वैवर्त में कृष्ण का राधा या अन्य गोपियों के साथ संभोग का जैसा वर्णन है, उसको पढ़कर उनके आचरण को अध्यात्म की भट्ठी में चाहे जितना तपाया जाये, उसे नैतिकता के मापदण्ड पर खरा नहीं ठहराया जा सकता।
मनु स्मृति संभवतः ऐसा अकेला ग्रन्थ है जिनसे भारतीय मेधा को न केवल सबसे अधिक आकर्षित किया अपितु व्यवहार-जगत् में उसकी मानसिकता को ठोस एवं स्थूल स्वरूप भी प्रदान किया। भारतीय मेधा अर्थात् भारतीय राज्य-सत्ता और उसके द्वारा पोषित सामंती प्रवृत्तियों का गंठजोड़, जिसके हाथ में मनु ने मनुस्मृति के रूप में, ‘करणीय और अकरणीय’ का औचित्य-विहीन संहिताकरण करके एक क्रूर और अमानवीय हथियार पकड़ा दिया और उसे धर्म-सम्मत मनमानी करने का निर्णायक अवसर प्रदान कर दिया। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मनुस्मृति का सबसे घातक दुष्परिणाम यह हुआ कि इसने पहले से ही क्षीण होती जा रही संतुलन-शक्तियों का समूल विनाश कर दिया। शूद्र (वर्तमान दलित) और स्त्री के लिये दंड-विधान के रूप में ऐसे-ऐसे प्रावधान किये गये कि इनका जीवन नारकीय हो गया।
विषय-वस्तु के बेहतर प्रतिपादन के लिये थोड़ा विषयान्तर समीचीन दिखता है। मनु-स्मृति में हमें तीन बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं। पहला, वर्ण-व्यवस्था का पूर्ण विकसित और अपरिवर्तनीय स्वरूप (मनु १०.४) दूसरा, राक्षस या असुर जाति का विलोपीकरण और तीसरा देवताओं के अनैतिक आचरण को विस्थापित करके उनकी कल्याणकारी इतर शक्तियों के रूप में स्थापना। वर्ण-व्यवस्था का सिद्धान्त आर्यों की देन है जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से प्रारम्भ होता है और सभी अनुवर्ती ग्रन्थों में जगह पाता है। स्त्रियों की भाँति राक्षसों की भी उत्पत्ति वर्ण-व्यवस्था से नहीं होती। सुर और असुर के मध्य लड़े गये तमाम युद्धों का वर्णन वैदिक साहित्य में भरे पड़े हैं। रामायण काल तक राक्षस मिलते हैं, महाभारत काल में विलुप्त हो जाते हैं। महाभारत काल में कृष्ण के रूप में ईश्वर अवतार लेते हैं। गीता में अपने अवतार का कारण अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना बताते हैं। प्रत्यक्ष विनाश वे अपने मामा कंस का करते है। महाभारत युद्ध की विनाश-लीला के नायक होते हुए भी इस युद्ध में उनकी भूमिका राम की तरह नहीं है। कृष्ण का मामा होने के कारण कंस को राक्षस कहा जाय तो सबसे बड़ी अड़चन यह आयेगी कि कृष्ण को भी राक्षस कहना पड़ेगा लेकिन थोड़ा-सा ध्यान दें तो इस गुत्थी को सुलझाना बहुत आसान है। राम और रावण के बीच लड़ा गया युद्ध निश्चित रूप से आर्यों के बीच लड़ा गया अन्तिम महायुद्ध था जिसमें आर्यों की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय यह थी कि आर्य राम की सेना अनार्य योद्धाओं की थी और रावण की पारिवारिक कलह चरम पर थी। इसका प्रत्यक्ष लाभ राम को यह मिला कि उन्हें घर का भेदी ही मिल गया और लंका ढह गयी। आर्य संस्कृति की विजय हुई लेकिन वर्चस्व स्थापित नहीं हो सका होगा। क्योंकि विभीषण चाहे जितना बड़ा राम भक्त राह हो, तो अनार्य ही न और फिर रावण की पटरानी मंदोदरी ही उसकी पटरानी बनी। क्या विभीषण कभी उससे आँख मिला पाया होगा? क्या कभी मंदोदरी यह भुला सकी होगी कि वह जिस कायर की पत्नी है उसी के विश्वासघात ने उसके प्रतापी पति की हत्या करवाई थी।
इस कड़ी को कृष्ण द्वारा कंस के संहार से जोड़कर देखें तो स्थिति यह बनती है कि अनार्यों की बची-खुची शक्ति के सम्पूर्ण विनाश के लिये इस बार घर से ही नायक को उठाया गया। यह इस बात से सिद्ध है कि कृष्ण के नायकत्व या संयोजकत्व में जितने भी युद्ध लड़े गये सभी पारिवारिक थे। अतः यह कहा जा सकता है कि अनार्य आपस में लड़कर विनाश को प्राप्त हुए और वर्ण से बाहर की दलित जातियाँ उन्हीं की ध्वंसावशेष हैं। इस सम्पूर्ण विजय के बाद आचरण हीन देवता स्वयं को कल्याणकारी इतर शक्ति के रूप में स्थापित कराने में सफल हो गये तो क्या आश्चर्य।
मनु स्मृति शांति काल की रचना प्रतीत होती है जिसमें शासन-व्यवस्था के संचालन और समाज को नियंत्रित करने का प्रावधान है। स्पष्ट है कि इसका डंडा वर्णेतर जातियों पर पड़ना था और पड़ा भी। दलित और स्त्री उन सभी सुविधाओं और अवसरों से वंचित कर दिये गये जो उनके बौद्धिक-क्षमता के विकास में सहायक थे। इस प्रकार मनु स्मृति से भी यह सिद्ध होता है कि दलित और स्त्री वर्ण-व्यवस्था के बाहर का समुदाय है।
मूलचंद जी के लेख से कुछ आगे जारी रखते हुए …….
अभी तो मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि स्त्री मर जाती है, स्त्री पैदा होती है लेकिन उसके दुर्गति की शाश्वतता बनी रहती है। इंतजार है नई स्त्री के पैदा होने की जो विद्रोह कर सके। ब्रह्मा, विष्णु और शिव हिन्दू धर्म में ईश्वर की तीन सर्वोच्च प्रतीक हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति, विष्णु पालन और शिव संहार के देवता माने गये हैं। इस रूप में ये एक-दूसरे के पूरक दिखते हैं लेकिन वैष्णवों के मध्य हुए संघर्षों से यह सिद्ध होता है कि प्रारम्भ के किसी काल-खंड में शिव और विष्णु एक-दूसरे के विरोधी विचारधारा के पोषक और संवाहक थे। पालक होते हुए भी तथाकथित अधर्मियों का विनाश करने के लिए विष्णु ही बार-बार अवतार लेते हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती इनकी पत्नियों के नाम हैं। आइये देखें कि यौन-विज्ञान के महारथियों ने इनका किस प्रकार चित्रण किया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का सरस्वती, लक्ष्मी और पर्वती के साथ पत्नी के अतिरिक्त अन्य सम्बन्ध का उल्लेख इस लेख के दूसरे खंड में किया जा चुका है। आगे बढ़ने से पूर्व स्त्रियों के प्रति इस वीभत्स काम-कुंठा की अभद्र मानसिकता की एक बानगी देखिये जो ‘खट्टर काका’ के अन्तिम पृष्ठ पर अथर्ववेद के हवाले से उद्धृत किया गया है-यावर्दैीनं पारस्वतं हास्तिनं गार्दभं च यत्/यावदश्वस्य वाजिनस्तावत् से वर्धतां पसः। (अथर्व ६/७२/३)
अर्थात् ‘‘कामदंड बढ़कर वैसा स्थूल हो जाय जैसा हाथी, घोड़े या गधे का…।”
इस लम्पट और उद्दंड कामुकता के वेग का प्रभाव ऐसा पड़ा यहाँ के यौनाचार्यों पर कि देवी तक की वंदना करते समय उनके कामांगों का स्मरण करना नहीं भूलते। उदाहरण-वामकुचनिहित वीणाम/वरदां संगीत मातृकां वंदे।
बायें स्तन पर वीणा टिकाये हुए संगीत की देवी की वंदना करते है। (खट्टर काका, पृष्ठ १६६)
स्मरेत् प्रथम पुष्पणीम्/रुधिर बिंदु नीलम्बराम्/घनस्तन भरोन्नताम्/त्रिपुर सुन्दरी माश्रये (खट्टर काका, पृष्ठ १६५)
‘प्रथम पुष्पिता होने के कारण जिनका वस्त्र रक्तरंजित हो गया है, वैसी पीनोन्नतस्तनी त्रिापुर सुन्दरी का आश्रय मैं ग्रहण करता हूँ।
कालतंत्र में काली का ध्यान-घोरदंष्ट्रा करालास्या पीनोन्नतपयोधरा/महाकालेन च समं विपरीतरतातुरा। (वही, पृष्ठ १६६)
कच कुचचिबुकाग्रे पाणिषु व्यापितेषु/प्रथम जलाधि-पुत्री-संगमेऽनंग धाग्नि/ग्रथित निविडनीवी ग्रन्थिनिर्मोंचनार्थं चतुरधिक कराशः पातु न श्चक्रमाणि। (वही, पृष्ठ १६७)
लक्ष्मी के साथ चतुर्भुज भगवान् का प्रथम संगम हो रहा है। उनके चारों हाथ फंसे हुए हैं। दो लक्ष्मी के स्तनों में, एक केश में, एक ठोढ़ी में। अब नीवी (साड़ी की गाँठ खोलें तो कैसे? इस काम के लिये एडीशनल हैंड (अतिरिक्त हाथ) चाहने वाले विष्णु भगवान् हम लोगों की रक्षा करें-पद्मायाः स्तनहेमसद्मनि मणिश्रेणी समाकर्षके/किंचित कंचुक-संधि-सन्निधिगते शौरेः करे तस्करे/सद्यो जागृहि जागृहीति बलयध्यानै र्ध्रुवं गर्जता/कामेन प्रतिबोधिताः प्रहरिकाः रोमांकुरः पान्तु नः।अर्थात् लक्ष्मी की कंचुकी में भगवान का हाथ घुस रहा है। यह देखकर कामदेव अपने प्रहरियों को जगा रहे हैं- उठो, उठो घर में चोर घुस रहा है। प्रहरी गण जागकर खड़े हो गये हैं। वे ही खड़े रोमांकुर हम लोगों की रक्षा करें। पार्वती की वंदना-गिरिजायाः स्तनौ वंदे भवभूति सिताननौ, तपस्वी कां गतोऽवस्थामिति स्मेराननाविव,….अंकनिलीनगजानन शंकाकुल बाहुलेयहृतवसनौ/समिस्तहरकरकलितौ हिमगिरितनयास्तनौ जयतः।(वही, पृष्ठ १६८)तो यह कामांध मस्तिष्क की वीभत्स परिणति जो देवी-देवताओं तक को नहीं छोड़ती लेकिन प्रचार किया जाता है कि देश की महान् संस्कृति स्त्रियों को पूज्य घोषित करती है
मूलचंद जी के लेख से कुछ आगे जारी रखते हुए …….
लेख के दूसरे भाग में वि.का. राजवाडे की पुस्तक ‘भारतीय विवाह संस्था का इतिहास’ के पृष्ठ १२८ से उद्धृत वाक्य को आपने देखा। इसी वाक्य के तारतम्य में ही आगे लिखा है, ‘‘यह नाटक होने के बाद रानी कहती है – महिलाओं, मुझसे कोई भी संभोग नहीं करता। अतएव यह घोड़ा मेरे पास सोता है।….घोड़ा मुझसे संभोग करता है, इसका कारण इतना ही है अन्य कोई भी मुझसे संभोग नहीं करता।….मुझसे कोई पुरुष संभोग नहीं कर रहा है इसलिए मैं घोड़े के पास जाती हूँ।” इस पर एक तीसरी कहती है – ‘‘तू यह अपना नसीब मान कि तुझे घोड़ा तो मिल गया। तेरी माँ को तो वह भी नहीं मिला।”
ऐसा है संभोग-इच्छा के संताप में जलती एक स्त्री का उद्गार, जिसे राज-पत्नी के मुँह से कहलवाया गया है। इसी पुस्तक के पृष्ठ १२६ पर अंकित यह वाक्य स्त्रियों की कामुक मनोदशा का कितना स्पष्ट विश्लेषण करता है, ‘‘बाद में प्रगति हासिल करके जब लोगों को अग्नि तैयार करने की प्रक्रिया का ज्ञान हुआ तब वे वन्य लोग अग्नि के आस-पास रतिक्रिया करते थे। किसी भी स्त्री को किसी भी पुरुष द्वारा रतिक्रिया के लिए पकड़कर ले जाना, उस काल में धर्म माना जाता था। यदि किसी स्त्री को, कोई पुरुष पकड़कर न ले जाए, तो वह स्त्री बहुत उदास होकर रोया करती थी कि उसे कोई पकड़कर नहीं ले जाता और रति सुख नहीं देता। इस प्रकार की स्त्री को पशु आदि प्राणियों से अभिगमन करने की स्वतंत्रता थी। वन्य ऋषि-पूर्वजों में स्त्री-पुरुष में समागम की ऐसी ही पद्धति रूढ़ थी।” यह कथन निर्विवाद रूप से स्त्रियों की उसी मानसिकता का उद्घाटन करता है कि वे संभोग के लिए न केवल प्रस्तुत रहती हैं, बल्कि उनका एकमात्र अभिप्रेत यौन-तृप्ति के लिए पुरुषों को प्रेरित करना है।
इस तरह के दृष्टांत वेद-पुराण इत्यादि में भी बहुततायत से उपलब्ध हैं। यहाँ ऋग्वेद के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं -
मेरे पास आकर मुझे अच्छी तरह स्पर्श करो। ऐसा मत समझना कि मैं कम रोयें वाली संभोग योग्य नहीं हूँ(यानी बालिग नहीं हूँ)। मैं गाँधारी भेड़ की तरह लोमपूर्णा (यानी गुप्तांगों पर घने रोंगटे वाली) तथा पूर्णावयवा अर्थात् पूर्ण (विकसित अधिक सटीक लगता है) अंगों वाली हूँ।(ऋ. १।१२६।७) (डॉ. तुलसीराम का लेख-बौद्ध धर्म तथा वर्ण-व्यवस्था-हँस, अगस्त २००४)
कोई भी स्त्री मेरे समान सौभाग्यशालिनी एवं उत्तम पुत्र वाली नहीं है। मेरे समान कोई भी स्त्री न तो पुरुष को अपना शरीर अर्पित करने वाली है और न संभोग के समय जाँघों को फैलाने वाली है।(ऋ. १०/८६/६) ऋग्वेद-डॉ. गंगा सहाय शर्मा, संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण १९८५)
हे इन्द्र! तीखे सींगों वाला बैल जिस प्रकार गर्जना करता हुआ गायों में रमण करता है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ रमण करो।(ऋ. १०/८६/१५) (वही)
ब्रह्म वैवर्त पुराण में मोहिनी नामक वेश्या का आख्यान है जो ब्रह्मा से संभोग की याचना करती है और ठुकराए जाने पर उन्हें धिक्कारते हुए कहती है, ‘‘उत्तम पुरुष वह है जो बिना कहे ही, नारी की इच्छा जान, उसे खींचकर संभोग कर ले। मध्यम पुरुष वह है जो नारी के कहने पर संभोग करे और जो बार-बार कामातुर नारी के उकसाने पर भी संभोग नहीं करे, वह पुरुष नहीं, नपुंसक है।(खट्टर काका, पृ. १८८, सं. छठाँ)
इतना कहने पर भी जब ब्रह्मा उत्तेजित नहीं हुए तो मोहिनी ने उन्हें अपूज्य होने का शाप दे दिया। शाप से घबराए हुए ब्रह्मा जब विष्णु भगवान से फ़रियाद करने पहुँचे तो उन्होंने डाँटते हुए नसीहत दिया, ‘‘यदि संयोगवश कोई कामातुर एकांत में आकर स्वयं उपस्थित हो जाए तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो कामार्त्ता स्त्री का ऐसा अपमान करता है, वह निश्चय ही अपराधी है। (खट्टर काका, पृष्ठ १८९) लक्ष्मी भी बरस पड़ीं, ‘‘जब वेश्या ने स्वयं मुँह खोलकर संभोग की याचना की तब ब्रह्मा ने क्यों नहीं उसकी इच्छा पूरी की? यह नारी का महान् अपमान हुआ।” ऐसा कहते हुए लक्ष्मी ने भी वेश्या के शाप की पुष्टि कर दी।(वही, पृष्ठ १८९)
विष्णु के कृष्णावतार के रूप में स्त्री-भोग का अटूट रिकार्ड स्थापित करके अपनी नसीहत को पूरा करके दिखा दिया। ब्रह्म वैवर्त में राधा-कृष्ण संभोग का जो वीभत्स दृश्य है उसका वर्णन डॉ. गंगासहाय ‘प्रेमी’ ने अपने लेख ‘कृष्ण और राधा’ में करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया इन शब्दों में व्यक्त किया है, ‘‘पता नहीं, राधा कृष्ण संभोग करते थे या लड़ाई लड़ते थे कि एक संभोग के बाद बेचारी राधा लहूलुहान हो जाती थी। उसके नितंब, स्तन और अधर बुरी तरह घायल हो जाते। राधा मरहम पट्टी का सामान साथ रखती होगी। राधा इतनी घायल होने पर प्रति रात कैसे संभोग कराती थी, इसे बेचारी वही जाने। (सरिता, मुक्ता रिप्रिंट भाग-२) इस प्रतिक्रिया में जो बात कहने को छूट गयी वह यह है कि इस हिंसक संभोग, जिसे बलात्कार कहना ज्यादा उचित है, से राधा प्रसन्न होती थी जिससे यही लगता है कि स्त्रियाँ बलात्कृत होना चाहती हैं।
History of prostitution in india के पृष्ठ १४७ पर पद्म पुराण के उद्धृत यह आख्यान प्रश्नगत प्रसंग में संदर्भित करने योग्य है। एक विधवा क्षत्राणी जो कि पूर्व रानी होती है, किसी वेद-पारंगत ब्राह्मण पर आसक्त होकर समर्पण करने के उद्देश्य से एकांत में उसके पास जाती है लेकिन ब्राह्मण इनकार कर देता है। इस पर विधवा यह सोचती है कि यदि वह उस ब्राह्मण के द्वारा बेहोशी का नाटक करे तो वह उसको ज+रूर अपनी बाँहों में उठा लेगा और तब वह उसे गले में हाथ डालकर और अपने अंगों को प्रदर्शित व स्पर्श कराकर उसे उत्तेजित कर देगी और अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगी। निम्न श्लोक उसकी सोच को उद्घाटित करते हैं – सुस्निग्ध रोम रहितं पक्वाश्वत्थदलाकृति।/दर्शयिष्यामितद्स्थानम् कामगेहो सुगन्धि च॥
मैं उसको पूर्ण विकसित पीपल के पत्ते की आकार की रोम रहित मृदुल और सुगंधित काम गेह(योनि) को (किसी न किसी तरह से) दिखा दूँगी क्योंकि – बाहूमूल कूचद्वंन्दू योनिस्पर्शन दर्शनात्।/कस्य न स्ख़लते चिन्तं रेतः स्कन्नच नो भवेत्॥
यह निश्चित है कि ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जिसका वीर्य किसी के बाहु-युगल, स्तन-द्वय और योनि को छूने और देखने से स्खलित न होता हो।
इससे ज्ञात होता है की आर्ष समाज से लेकर अर्वाचीन समाज तक स्त्रियों की छवि को एक विशेष खाँचे में फिट किया गया है, मातृ-सत्तात्मक समाज रहा हो या पितृ-सत्तात्मक स्त्री को देह की भाषा में ही व्यक्त करने और होने का खेल चलता रहा। और स्त्री को पूजा जाता है ये बकवास की जाती रही है ………………………..
परन्तु अब ये sambhav nahi reh gaya है
मूलचन्द सोनकर ji ke lekh ke ansh
पा.ना. सुब्रमणियन द्वारा लिखा एक लेख है जिसके कुछ अंश इस दिशा में सहायक सिद्ध होंगे की नारी का कितना सम्मान किया जाता रहा है ………………..
कदम्ब वंशीय राजा मयूर शर्मन के समय सर्वप्रथम केरल में ब्राह्मणों का आगमन हुआ. उसके पहले वहां बौद्ध एवं जैन धर्म का बोलबाला रहा. कुछ ब्राह्मण पंडितों ने शास्त्रार्थ कर वहां के बौद्ध भिक्षुओं को परास्त कर दिया. शंकराचार्य (७८८-८२०) के नेतृत्व में हिंदू/सनातन धर्म के पुनरूत्थान के प्रयास स्वरुप शनै शनै बौद्ध तथा जैन धर्म के अनुयायी कम होते चले गए. चेर वंश के कुलशेखर राजाओं (८०० – ११००) ने भी ब्राह्मणों को प्राश्रय और प्रोत्साहन दिया. कहते हैं कि जो ब्राह्मण उत्तर दिशा से आए उन्हें केरल के ३२ और कर्णाटक के तुलुनाडु के ३२ गांवों में बसाया गया था. यही वहां के नम्बूतिरी ब्राह्मण कहलाते हैं जो अपने आपको स्थानीय कहते हैं. कालांतर में इन्हीं ब्राह्मणों में उपलब्ध भूमि आबंटित कर दी गई थी और एक तरह से वे ही वहां के जमींदार बन बैठे. वे जमीन पट्टे पर दूसरों को खेती या अन्य प्रयोजन के लिए दे दिया करते और एवज में उन्हें वार्षिक भू राजस्व की प्राप्ति होती थी. (कृषि उत्पाद या तरल मुद्रा के रूप में)
नम्बूतिरी ब्राह्मणों के निवास को “मना” और कुछ जगह “इल्लम” कह कर पुकारते है. ये साधारणतया एक बड़े भूभाग पर आलीशान बने होते हैं. इसी के अन्दर सेवकों आदि के निवास की भी व्यवस्था होती थी. नाम्पूतिरी लोग भी उत्तर भारतीय पंडितों की तरह चुटैय्या धारण करते थे लेकिन इनकी चोटी पीछे न होकर माथे के ऊपर कोने में हुआ करती थी. इष्ट देव की आराधना में मन्त्र के अतिरिक्त तंत्र की प्रधानता होती है. पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी केवल ज्येष्ठ पुत्र ही हुआ करता था और वही एक मात्र व्यक्ति विवाह करने का भी अधिकारी होता था. पत्नियों की संख्या चार तक हो सकती थी (Polygamy). परिवार के सभी सदस्य एक साथ “मना” में ही निवास करते थे. इस व्यवस्था से संपत्ति विघटित न होकर यथावत बनी रहती थी. अब परिवार के जो दूसरे युवा हैं उन्हें इस बात की स्वतंत्रता दी गई थी कि वे चाहें तो बाहर किसी अन्य ज़ाति (क्षत्रिय अथवा शूद्र) की महिलाओं, अधिकतम चार से “सम्बन्ध” बना सकते थे. ऐसे सम्बन्ध अधिकतर अस्थायी ही होते थे. “सम्बन्ध” बनने के लिए पसंदीदा स्त्री को भेंट स्वरुप वस्त्र (केवल एक गमछे से काम चल जाता था) दिए जाने की परम्परा थी. वस्त्र स्वीकार करना “सम्बन्ध” की स्वीकारोक्ति हो जाया करती थी. जिस महिला से “सम्बन्ध” बनता था, उसके घर रहने के लिए रात में जाया करते और सुबह उठते ही वापस अपने घर “मना” आ जाते. रात अंधेरे में सम्बन्धम के लिए जाते समय अपने साथ एक लटकने वाला दीप भी ले जाते, जिसकी बनावट अलग प्रकार की होती थी और इसे “सम्बन्धम विलक्कू” के नाम से जाना जाता था.
नम्बूतिरी ब्राह्मणों की इस सामाजिक व्यवस्था के परिणाम स्वरुप जहाँ उनकी आबादी कम होती चली गई, वहीं दूसरी तरफ़ योग्य वर के न मिल पाने के कारण कई नम्बूतिरी कन्यायें अविवाहित ही रह जाती. अंततोगत्वा भारत में हिन्दुओं के लिए समान/सार्वजनिक विवाह और उत्तराधिकार नियम बन जाने से उनकी रुढिवादी परम्पराओं का अंत हुआ. केरल में १९६५-७० में भूमि सुधार कानूनों के लागू होने से नम्बूतिरी घरानों की सम्पन्नता भी जाती रही.
केरल के समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग नायरों (इसमे पिल्लई, मेनोन, पणिक्कर, मारार, नम्बियार, कुरूप आदि लोग भी शामिल हैं) का था. तकनीकी दृष्टि से ये शूद्र थे परन्तु योद्धा हुआ करते थे. सेना में ये कार्यरत होते थे अतः क्षत्रिय सदृश माना जा सकता है. इनके समाज में अधिकार स्त्रियों के हाथों हुआ करता था. उत्तराधिकार के नियम आदि स्त्रियों पर केंद्रित थे. इस व्यवस्था को “मरुमक्कतायम” कहा जाता था. इन लोगों में विवाह नामकी कोई संस्था नहीं थी. घर की लड़कियां अपने अपने घरों (जिन्हें “तरवाड़” कहा जाता है) में ही रहतीं. सभी भाई बहन इकट्ठे अपनी माँ के साथ. घर के मुखिया के रूप में मामा(मुजुर्ग महिला का भाई) नाम के लिए प्रतिनिधित्व करता था. किसी कन्या के रजस्वला होने पर किसी उपयुक्त पुरूष की तलाश होती जिस के साथ “सम्बन्धम” किया जा सके. यहीं नम्बूतिरी ब्राहमणों का काम बन जाता था क्योंकि कई विवाह से वंचित युवक किसी सुंदर कन्या से संसर्ग के लिए लालायित रहते थे . नायर परिवार में “सम्बन्धम” के लिए नम्बूतिरी या अन्य ब्राह्मण पहली पसंद होती थी क्योंकि उन्हें बुद्धिमान समझा जाता था. जैसे नम्बूतिरी घरों के युवकों को चार स्त्रियों से सम्बन्धम की अनुमति थी वैसे ही यहाँ नायर समुदाय की स्त्रियों के लिए भी आवश्यक नहीं था कि वे केवल एक से ही सम्बन्ध बनाये रखें. एक से अधिक (Polyandry) भी हो सकते थे. अंशकालिक!. सम्बन्धम, जैसा पूर्व में ही कहा जा चुका है, साधारणतया अस्थायी पाया गया है. लेकिन स्थायी सम्बन्धम भी होते थे, किसी दूसरे संपन्न तरवाड़ के नायर युवक से. कभी कभी एक स्थाई और कुछ दूसरे अस्थायी/ अंशकालिक. एक से अधिक पुरुषों से सम्बन्ध होने की स्थिति में समय का बटवारा भी होता था. पुरूष रात्रि विश्राम के लिए स्त्री के घर आता और सुबह उठते ही अपने घर चला जाता. संतानोत्पत्ति के बाद बच्चों की परवरिश का कोई उत्तरदायित्व पुरूष का नहीं रहता था. सब “तरवाड़” के जिम्मे. परिवार की कन्याओं का सम्बन्ध धनी नम्पुतिरियों से रहने के कारण धन “मना” से “तरवाड़” की और प्रवाहित होने लगा और “तरवाड़” धनी होकर प्रतिष्ठित हो गए. कुछ तरवाडों की प्रतिष्ठा इतनी रही कि वहां की कन्याओं से सम्बन्ध बनना सामाजिक प्रतिष्ठा का भी द्योतक रहा.
नायरों जैसी ही स्थिति राज परिवारों की भी रही. उनकी कन्याओं का सम्बन्ध किसी दूसरे राज परिवार के पुरूष या किसी ब्राह्मण से हो सकता था और राज परिवार के युवकों का सम्बन्ध नायर परिवार की कन्याओं के साथ.
यहाँ यह बताना उचित होगा कि इस पूरी व्यवस्था को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी और किसी भी दृष्टिकोण से इसे हेय नहीं समझा जाता था.
Friday, September 24, 2010
नारी की पूजा इस देश में कहीं भी न तो पूजा की जाती है, न की जाती थी।
 जहाँ तक नारी या स्त्री की पूजा की जाने की बात है तो पहली बात तो ये कि नारी की इस देश में कहीं भी न तो पूजा की जाती है, न की जाती थी। केवल नारी प्रतिमा दुर्गा देवी, कालिका देवी आदि अनेकों नामों से देवियों के रूप में पूजा अवश्य की जाती रही है।
जहाँ तक नारी या स्त्री की पूजा की जाने की बात है तो पहली बात तो ये कि नारी की इस देश में कहीं भी न तो पूजा की जाती है, न की जाती थी। केवल नारी प्रतिमा दुर्गा देवी, कालिका देवी आदि अनेकों नामों से देवियों के रूप में पूजा अवश्य की जाती रही है।मनु महाराज के जिस एक श्लोक (यत्र नार्यस्त पूज्यंते रमन्ते तत्र देवताः) के आधार पर नारी की पूजा की बात की जाती रहती है, लेकिन उन्हीं मनुमहाराज की एवं अन्य अनेक धर्मशास्त्रियों/धर्मग्रन्थ लेखकों की बातों को हम क्यों भुला देते हैं? इनको भी जान लेना चाहिये :-
मनुस्मृति : ९/३-
स्त्री सदा किसी न किसी के अधीन रहती है, क्योंकि वह स्वतन्त्रता के योग्य नहीं है।
मनुस्मृति : ९/११-
स्त्री को घर के सारे कार्य सुपुर्द कर देने चाहिये, जिससे कि वह घर से बाहर ही नहीं निकल सके।
मनुस्मृति : ९/१५-
स्त्रियाँ स्वभाव से ही पर पुरुषों पर रीझने वाली, चंचल और अस्थिर अनुराग वाली होती हैं।
मनुस्मृति : ९/४५-
पति चाहे स्त्री को बेच दे या उसका परित्याग कर दे, किन्तु वह उसकी पत्नी ही कहलायेगी। प्रजापति द्वारा स्थापित यही सनातन धर्म है।
मनुस्मृति : ९/७७-
जो स्त्री अपने आलसी, नशा करने वाले अथवा रोगग्रस्त पति की आज्ञा का पालन नहीं करे, उसे वस्त्राभूषण उतार कर (अर्थात् निर्वस्त्र करके) तीन माह के लिये अलग कर देना चाहिये।
आठवीं सदी के कथित महान हिन्दू दार्शनिक शंकराचार्य के विचार भी स्त्रियों के बारे में जान लें :-
“नारी नरक का द्वार है।”
तुलसी ने तो नारी की जमकर आलोचना की है, कबीर जैसे सन्त भी नारी का विरोध करने से नहीं चूके :-
नारी की झाईं परत, अंधा होत भुजंग।
कबिरा तिन की क्या गति, नित नारी के संग॥
अब आप अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहे जाने वाले कौटिल्य (चाणक्य) के स्त्री के बारे में प्रकट विचारों का अवलोकन करें, जो उन्होंने चाणक्यनीतिदर्पण में प्रकट किये हैं :-
चाणक्यनीतिदर्पण : १०/४-
स्त्रियाँ कौन सा दुष्कर्म नहीं कर सकती?
चाणक्यनीतिदर्पण : २/१-
झूठ, दुस्साहस, कपट, मूर्खता, लालच, अपवित्रता और निर्दयता स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं।
चाणक्यनीतिदर्पण : १६/२-
स्त्रियाँ एक (पुरुष) के साथ बात करती हुई, दूसरे (पुरुष) की ओर देख रही होती हैं और दिल में किसी तीसरे (पुरुष) का चिन्तन हो रहा होता है। इन्हें (स्त्रियों को) किसी एक से प्यार नहीं होता।
पंचतन्त्र की प्रसिद्ध कथाओं में शामिल शृंगारशतक के ७६ वें प में स्त्री के बारे में लिखा है कि-
“स्त्री संशयों का भंवर, उद्दण्डता का घर, उचित अनुचित काम (सम्भोग) की शौकीन, बुराईयों की जड, कपटों का भण्डार और अविश्वास की पात्र होती है। महापुरुषों को सब बुराईयों से भरपूर स्त्री से दूर रहना चाहिये। न जाने धर्म का संहार करने के लिये स्त्री की रचना किसने कर दी!”
मेरा तो ऐसा अनुभव है कि इस देश के कथित धर्मग्रन्थों और आदर्शों की दुहाई देने वाले पुरुष प्रधान समाज और धर्मशास्त्रियों ने अपने नियन्त्रण में बंधी हुई स्त्री को दो ही नाम दिये हैं, या तो दासी (जिसमें भोग्या और कुल्टा नाम भी समाहित हैं) जो स्त्री की हकीकत बना दी गयी है, या देवी जो हकीकत नहीं, स्त्री को बरगलाये रखने के लिये दी गयी काल्पनिक उपमा मात्र हैं।
स्त्री को देवी मानने या पूजा करने की बात बो बहुत बडी है, पुरुष द्वारा नारी को अपने बराबर, अपना दोस्त, अपना मित्र तक माना जाना भारतीय समाज में निषिद्ध माना जाता रहा है?
जब भी दो विषमलिंगी समाज द्वारा निर्धारित ऐसे स्वघोषित खोखले आदर्शवादी मानदण्डों पर खरे नहीं उतर पाते हैं, जिन्हें भारत के इतिहास में हर कालखण्ड में समर्थ लोगों द्वारा हजारों बार तोडा गया है तो भी 21वीं सदी में भी केवल नारी को ही पुरुष की दासी या कुल्टा क्यों माना जाता है? पुरुष के लिये भी तो कुछ उपमाएँ गढी जानी चाहिये! भारत में नारी की पूजा की जाती है, इस झूठ को हम कब तक ढोते रहना चाहते हैं?
Thursday, September 2, 2010
अम्बेडकर-मिशन के प्रचार व प्रसार ख़तरनाक और दुखदायक है।

समर्पण
डा. अम्बेडकर के इस संसार से विदा होने पर मेरे सार्वजनिक जीवन का आरम्भ हुआ। चालीस वर्ष पूर्व, जब ,
मैंने 6 दिसम्बर,1956 को सरकारी नौकरी त्याग कर अम्बेडकर-मिशन के प्रचार व प्रसार का बीड़ा उठाया तो यह गुमान भी न था कि मार्ग इतना कठिन है, ऐसा ख़तरनाक और दुखदायक है।
इन वर्षों में वह कौन सी आफ़त है जो मुझ पर नहीं टूटी। हवालात व जेल के दुख झेले, सरकारी और ग़ैर सरकारी मुक़द्दमों की परेशानियां सहन कीं। कभी अपनों का परायापन, कभी साथियों का विश्वासघात, तो कभी साधनहीनता के थपेड़े। यही सदा महसूस हुआ कि सुख-चैन मिलने का नहीं।
कुछ ही वर्षों में वह दौर बीत गया, फिर एक नया दौर शुरू हुआ, कर्तव्य पालन के इश्क ने संघर्ष से मुहब्बत पैदा की, विपरीत हालात ने दृढ़ता को जन्म दिया,दृढ़ता ने साहस को और फिर साहस ने सुख और दुख के बीच के सभी भेद मिटा डाले -
दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है
मौत मिले तो मुफ़्त न लूं हस्ती की क्या हस्ती है
फ़ानी बदायंूनी
इस अवस्था तक पहुंचने में जिस ने मेरा हाथ स्नेहपूर्ण मजबूती से निरन्तर थामे रखा जिन्होंने बंगलूर(कर्नाटक राज्य)
में भीमराव अम्बेडकर की याद को चिरस्थायी बनाने और साधनहीन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मैडिकल, डेंटल और इंजिनियरिंग कालेजों, स्कूलों, अनेकों होस्टलों की स्थापना की, अपने उसी
गुरूभाई श्री एल. शिवालिंगईया साहिब
को यह रचना सादर समर्पित है।
From Hinduism : Dharm ya Kalank
डा. अम्बेडकर के इस संसार से विदा होने पर मेरे सार्वजनिक जीवन का आरम्भ हुआ। चालीस वर्ष पूर्व, जब ,
मैंने 6 दिसम्बर,1956 को सरकारी नौकरी त्याग कर अम्बेडकर-मिशन के प्रचार व प्रसार का बीड़ा उठाया तो यह गुमान भी न था कि मार्ग इतना कठिन है, ऐसा ख़तरनाक और दुखदायक है।
इन वर्षों में वह कौन सी आफ़त है जो मुझ पर नहीं टूटी। हवालात व जेल के दुख झेले, सरकारी और ग़ैर सरकारी मुक़द्दमों की परेशानियां सहन कीं। कभी अपनों का परायापन, कभी साथियों का विश्वासघात, तो कभी साधनहीनता के थपेड़े। यही सदा महसूस हुआ कि सुख-चैन मिलने का नहीं।
कुछ ही वर्षों में वह दौर बीत गया, फिर एक नया दौर शुरू हुआ, कर्तव्य पालन के इश्क ने संघर्ष से मुहब्बत पैदा की, विपरीत हालात ने दृढ़ता को जन्म दिया,दृढ़ता ने साहस को और फिर साहस ने सुख और दुख के बीच के सभी भेद मिटा डाले -
दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है
मौत मिले तो मुफ़्त न लूं हस्ती की क्या हस्ती है
फ़ानी बदायंूनी
इस अवस्था तक पहुंचने में जिस ने मेरा हाथ स्नेहपूर्ण मजबूती से निरन्तर थामे रखा जिन्होंने बंगलूर(कर्नाटक राज्य)
में भीमराव अम्बेडकर की याद को चिरस्थायी बनाने और साधनहीन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मैडिकल, डेंटल और इंजिनियरिंग कालेजों, स्कूलों, अनेकों होस्टलों की स्थापना की, अपने उसी
गुरूभाई श्री एल. शिवालिंगईया साहिब
को यह रचना सादर समर्पित है।
From Hinduism : Dharm ya Kalank
Thursday, July 29, 2010
यदि विश्व में सोने के तख्त पर कोई व्यक्ति बैठता है तो वह एक व्यक्ति भारत का गुरू शंकराचार्य ही है।
 ऐसा नहीं है कि हमारा देश भुखमरों का देश है इसलिए भुखमरी है, गरीबों का देश है इसलिए गरीबी है और लाचारी व बेरोजगारों का देश है इसलिए लाचारी व बेरोजगारी है। इसके विपरीत तथ्य यह है कि हमारे देश में 15 प्रतिशत लोगों के पास इतना धन , इतना सोना, और इतना बैंक जमा है कि विश्व के पचासों देशों की पूरी जनसंख्या के पास होगा। हमारा देश कर्ज में डूबा है परंतु हमारे देश के इन 15 प्रतिशत (सवर्णों) के विदेशी खाते में जमा धन के ब्याज से ही भारत का पूरा कर्जा एक साल में उतर सकता है।
ऐसा नहीं है कि हमारा देश भुखमरों का देश है इसलिए भुखमरी है, गरीबों का देश है इसलिए गरीबी है और लाचारी व बेरोजगारों का देश है इसलिए लाचारी व बेरोजगारी है। इसके विपरीत तथ्य यह है कि हमारे देश में 15 प्रतिशत लोगों के पास इतना धन , इतना सोना, और इतना बैंक जमा है कि विश्व के पचासों देशों की पूरी जनसंख्या के पास होगा। हमारा देश कर्ज में डूबा है परंतु हमारे देश के इन 15 प्रतिशत (सवर्णों) के विदेशी खाते में जमा धन के ब्याज से ही भारत का पूरा कर्जा एक साल में उतर सकता है।हमारे देश में 10 लाख मंदिर हैं जो अरबों-खरबों के सोने चांदी और अनेक आभूषणों से भरे पड़े हैं। यदि विश्व में सोने के तख्त पर कोई व्यक्ति बैठता है तो वह एक व्यक्ति भारत का गुरू शंकराचार्य ही है। कुछ समय पूर्व अभी एक शंकराचार्य की मृत्यु हुई थी तो उसका शव भी सोने के तख्त पर लिटाया गया था। भारत में 5 प्रतिशत उच्च जातीय जमींदार हैं जिनमें एक-एक के पास 10-10 हजार एकड़ भूमि के फ़ार्म हैं। इन जमींदारों के पास भी अरबों-खरबों की सम्पत्ति है। इनमें कुछ राज-घराने के लोग हैं जिनके पास अब भी अरबों-खरबों के खजाने हैं, स्वर्ण महल हैं और निजी हवाई जहाज हैं। ये जमींदार और सामन्त अपनी बेटी और बेटे के विवाहों में रत्न जड़ित गलीचों का बिछोना बिछाते हैं।
भारत का वैश्य वर्ग भी कम नहीं है। वह सुई से लेकर रेल, हवाई जहाज तक का उद्योग चलाता है। सोना-चांदी, हीरे जवाहरात , तस्करी का माल, गाय की चर्बी और जीवित इन्सानी बच्चों तथा स्त्रियों के साथ ही वह आदमी के खून तक की तिजारत करता है। खाद्य-पदार्थों, दवाओं और जहर तक में मिलावट कर धन बटोरता है। आज देश की एक तिहाई पूंजी उसके पास है।
सच यह है कि हमारा 85 प्रतिशत भारत गरीब है, भूखा है, नंगा है, बेघरबार है और लाचार है पर 15 प्रतिशत सवर्ण लोग धन की उबकाई करते हैं और इनके कुत्ते कारों में सफर करते हैं, पांच सितारा होटलों में पुडिंग और मलाई खाते हैं जिसकी उन्हें बदहजमी हो जाती है। भारत के भूगोल में जहां एक तरफ शहरी कूड़े-करकट के ढेरों के बीच सड़े गले प्लास्टिक और फूंस से ढकी मिट्टी या बांस के खम्बों की खड़ी दलितों की झोंपड़ियां हैं तो दूसरी ओर वहीं हिन्दुओं की बहुमंजिली इमारतें, ऊंचे-ऊंचे रंगमहल और शीशमहल बने हुए हैं। एक तरफ पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी भी पर्याप्त नहीं है तो दूसरी ओर हिन्दुओं के ऊंचे-ऊंचे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, दुकानें, कारखाने हैं और भूमि के हजारों-हजारों एकड़ फार्म हैं। एक तरफ जहां दलितों का अपना कोई प्राइमरी स्कूल तक नहीं है वहीं दूसरी ओर हिन्दुओं के अपने डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। एक तरफ दलित गरीब के पास चलाने को टूटी साइकिल भी नहीं है तो दूसरी ओर एक-एक हिन्दू, सेठ, साहब और सन्यासी के पास 50-50 काफिलों में चलने वाली विलायती कारें हैं। दलित दरिद्र के मनोंरंजन का साधन मात्र उसकी पत्नी और उसके बच्चे हैं, जबकि हिन्दू महन्त, मठाधीश, ज़मींदार, शरमाएदार और सेठ चोटी से पैर तक अय्यासी में डूबे हुए रहते हैं। एक तरफ दलित मासूम बच्चों को 40-40 रूपये में पेट की खातिर बाजार में बेच देते हैं वहीं इन हिन्दुओं के अपने मसाजघर, मनोरंजन थियेटर, नाचघर, जुआघर और मयखाने हैं जहां जीवित मांस का व्यापार होता है।
हमारा देश गरीब है यह चीख-पुकार एक नाटक है, लाचारी है, हमारे देश में बेरोजगारी है यह भी एक नाटक है। गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी किसी देश में तब कही जा सकती है जब गरीबी, बेरोजगारी , लाचारी और भुखमरी से सब प्रभावित हों। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे यहां करोड़ों गरीब हैं और करोड़ों नंगे भी हैं। सच यह है कि हमारे यहां 15 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो सोना खाते हैं और सोने का ही वमन करते हैं। यहां मूल समस्या समाज में हिस्सेदारी की है। यदि 15 प्रतिशत के पास जमा सोना-चांदी, हीरे-जवाहरात के धन में हिस्सेदारी कर दी जाये तो भारत में एक भी व्यक्ति न भूखा सो सकता है न एक भी व्यक्ति नंगा रह सकता है। तब एक भी व्यक्ति न बेघरबार रह सकता है और न तब एक भी व्यक्ति बेरोजगार रह सकता है। यदि धर्मालयों का धन बाहर निकाल दिया जाय, भूमि का भूमिहीनों में वितरण कर दिया जाय और उद्योगों के लाइसेंस में एक व्यक्ति एक उद्योग कर दिया जाए तो हर तबाही तुरन्त दूर हो सकती है अथवा देवालयों, भूमि और उद्योग-व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो हमारा देश 132 वें स्थान से उठकर आज ही 32 वें स्थान पर आ सकता है।
देश की इस गर्दिश के लिए कौन उत्तरदायी है यह एक खुली किताब है। यह इन मुठ्ठी भर उच्च हिन्दुओं की स्वार्थ, शोषण दमन और भेदभावपूर्ण नीति का परिणाम है।
-पृ. 1-3, हिन्दू विदेशी हैं, लेखक एस.एल.सागर, सागर प्रकाशन 223 दरीबा,मैनपुरी, उ.प्र., द्वितीय संस्करण 1999 से साभार
Wednesday, July 28, 2010
डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म क्यों त्यागा ?
 ‘‘इस प्रश्न का उत्तर सरल है। यह जटिल विषय नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं डॉ. अम्बेडकर एक अछूत परिवार में जन्मे थे। इस तरह उन्हें व्यक्तिगत कडुवे और विकट अनुभव का ज्ञान था कि सवर्ण हिन्दू जातियों द्वारा उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाना कैसा लगा। उन्होंने यह भी देखा कि उनका अनुभव अपूर्व नहीं था, बल्कि भारत भर में करोड़ों अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। बहुत वर्षों तक डॉ. अम्बेडकर ने सवर्ण हिन्दुओं को अपना व्यवहार बदलने और इसमें सुधार लाने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अन्ततः वे इस नतीजे पर पहुंचे कि कम से कम व्यवहारिक रूप में हिन्दू धर्म और छूतछात एक दूसरे से अलग होने वाले नहीं हैं, और यदि कोई मनुष्य अपने आपको छुआछूत की दुर्गति से मुक्त करवाना चाहता है, जाति-पांति की लानत से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे हिन्दू मत को एकदम तिलांजलि देनी होगी। इसलिए 1935 में उन्होंने ऐलान किया,
‘‘इस प्रश्न का उत्तर सरल है। यह जटिल विषय नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं डॉ. अम्बेडकर एक अछूत परिवार में जन्मे थे। इस तरह उन्हें व्यक्तिगत कडुवे और विकट अनुभव का ज्ञान था कि सवर्ण हिन्दू जातियों द्वारा उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाना कैसा लगा। उन्होंने यह भी देखा कि उनका अनुभव अपूर्व नहीं था, बल्कि भारत भर में करोड़ों अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। बहुत वर्षों तक डॉ. अम्बेडकर ने सवर्ण हिन्दुओं को अपना व्यवहार बदलने और इसमें सुधार लाने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अन्ततः वे इस नतीजे पर पहुंचे कि कम से कम व्यवहारिक रूप में हिन्दू धर्म और छूतछात एक दूसरे से अलग होने वाले नहीं हैं, और यदि कोई मनुष्य अपने आपको छुआछूत की दुर्गति से मुक्त करवाना चाहता है, जाति-पांति की लानत से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे हिन्दू मत को एकदम तिलांजलि देनी होगी। इसलिए 1935 में उन्होंने ऐलान किया,‘यद्यपि मैं हिन्दू जन्मा हूं , मैं हिन्दू मरूंगा नहीं।‘
संक्षेप में , यही कारण था कि डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म को त्यागा। उन्होंने देखा कि हिन्दू धर्म में अछूत के रूप में पैदा हुए मनुष्य के लिए मानव की तरह सुशीलता और शान से जीवन व्यतीत करना असम्भव है।‘‘
डॉ. अम्बेडकर की सच्ची महानता : संघरक्षित, पृष्ठ 32 से साभार
Subscribe to:
Comments (Atom)